अनुवाद की संकल्पना में संज्ञा की अनुवादनीयता का प्रश्न
(हिंदी से अनुवाद करने के विशेष संदर्भ में)
शिवानी पंवार
शोधार्थी पीएच्.डी. (हिंदी)
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़
shivani.panwar11@gmail.com
अनुवाद करते समय साहित्य की समतुल्यता एवं अनुवादनीयता का विशेष महत्त्व है। प्रत्येक स्थान की भाषा एवं साहित्य स्वंय में विलक्षण होता है, जो अपने अंदर क्षेत्र एवं समाज के गूढ़ अर्थों को समेटे रहती है। संज्ञा का अनुवाद करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। जिसका अनुवादक को विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे वह मूल रचना, रचनाकार एवं अनूदित पाठ के पाठकों के साथ पूर्ण न्याय कर सके। अनुवाद का मूलाधारित एवं बोधगम्य होना उसकी आवश्यक होता है। जिसके लिए अनुवादक को संज्ञा के अनुवाद में लिपियंतरण, रूपांतरण एवं स्थानांतरण आदि की सहायता ले लेनी चाहिए।
बीज शब्द : अनुवादनीयता, समतुल्यता, बोधगम्य, लिपियन्तरण
शोध आलेख
अनुवाद शब्द का जो अर्थ हमें आज देखने को मिलता है, प्राचीन समय में अनुवाद शब्द का वह तात्पर्य नहीं था। एक लंबी यात्रा करने के बाद आज यह अपने वर्तमान रूप में पहुंचा है। “भारत में अनुवाद के प्रारंभ की बात करें तो हम देखते हैं कि अनुवाद संस्कृत भाषा का तत्सम शब्द है, ‘अनुवाद’ अनु (पीछे) वद् (बोलना) से उत्पन्न हुआ है। जिससे तात्पर्य पुनरुक्ति, अर्थात् किसी बात को फिर से कहना।
“अन्वेको वदति यद्दाति तद्रूपा मिनन्तदपा एक ईयते।
विश्वा एकस्य विनुदस्तितिक्षते यस्ताकृणो: प्रथमं सास्युकथ्य॥” 1
इसमें ‘अनु- वदति’ का प्रयोग दुहराने या पीछे से कहने के अर्थ में हुआ है। किसी वक्तव्य का एक भाषा से दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना जैसा अर्थ संस्कृत में प्रचलित नहीं रहा होगा। भारतीय संदर्भ की बात करें तो अनुवाद का प्रारंभिक स्वरूप हमें गुरुकुल आश्रमों में दिखायी पड़ता है। जब गुरु के मंत्र, कथ्य को शिष्य दोहराते थे। इस प्रकार अनुवाद शब्द से अर्थ लिया जाता है – किसी कही गयी बात को फिर से कहना। अनुवादक मूलरचना के संदेश को यथारूप में ‘लक्ष्यभाषा’ में अभिव्यक्त करता है। उसको मूल रचना की विषयवस्तु और रचना शैली की रक्षा करते हुए अनूदित पाठ को बोधगम्य एवं सहज बनाने के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बशर्ते मूलरचना को कोई ह्रास न हो। अनुवाद शब्द के लिए अंग्रेज़ी भाषा में ‘Translation’ शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। जिसका निर्माण दो शब्दों ‘Trans’ एवं ‘Lation’ के योग से हुआ है । Trans का अर्थ है ‘पार’ और Lation का अर्थ है ‘नयन’। इस प्रकार Translation का अर्थ है ‘एक पार से दूसरे पार ले जाने की क्रिया।’2
स्रोत भाषा की अभिव्यक्ति के विभिन्न आयाम अथवा स्तर हो सकते हैं। यह मूल रचना के ध्वनि, लय, लिपि के साथ-साथ भाषा की संस्कृति में गर्भित विभिन्न अर्थों को अभिव्यक्त करती है। इसका स्वरूप स्वंय में भिन्न होता है। इसे दूसरी भाषा में स्थानांतरित करना कठिन कार्य है। “भाषा की प्रकृति ऐसी स्थिर, निष्क्रिय और समरूपी नहीं है कि एक भाषा की इकाई का दूसरी भाषा की इकाई में प्रतिस्थापन या अंतरण किया जा सके। भाषा ऐसी निष्क्रिय, ग्रहीता नहीं है और न ही सामान्य माध्यम या उपकरण है जो किसी अन्य भाषा के कथ्य को बिना किसी टकराव या संघर्ष के अपने भीतर समेट ले।”3
प्रत्येक भाषा का संबंध उसके स्थान एवं देशकाल से जुड़ा होता है, जो भाषा की सरंचना में घर किये रहता है। भाषा के प्रसंगों का संबंध भाषा के लाक्षणिक तथा व्यंजनात्मक रूप एवं उससे जुड़े स्थानिक, देशकाल से होता है तथा संदर्भ का संबंध भाषा में निहित गहरे सांस्कृतिक संदर्भों से होता है। इसलिए शब्द का संबंध मात्र कोशगत न होकर, वह प्रसंग एवं संदर्भगत भी होता है। इसी के साथ अनुवादक को शब्द की उत्पत्ति, सामाजिक स्थिति एवं युग की अच्छी पहचान होना आवश्यक है। “भाषिक प्रतीक में बाह्य-जगत की वस्तुओं के साथ-साथ प्रयोक्ता के जातीय इतिहास, उसकी सभ्यता, उसके समाज और संस्कृति का भी योगदान रहता है। इसी कारण संकेतार्थ में, अर्थ में असीम संभावनाएँ निहित रहती हैं, जो मुख्यतः बोधात्मक या कोशगत अर्थ, संरचनात्मक अर्थ, सामाजिक-सांस्कृतिक अर्थ और लाक्षणिक एवं व्यंजनापरक अर्थ को अपने भीतर समेटे रहती है।”4
अनुवाद में अनुवादनीयता एवं समतुल्यता का विशेष महत्त्व है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अनुवादनीयता से तात्पर्य है – किसी भाषा या उसके वक्तव्य अथवा इकाई शब्द का अनुवाद किस स्तर तक किया जा सकता है। वही समतुल्यता वह साधन है जिसके आधार पर हम मूल एवं अनूदित पाठ के प्रभाव का आकलन करते हैं। यह आकलन शब्द, अर्थ, व्याकरण, लय, तरतम्यता, बोधगम्यता, प्रभाव आदि सभी को ध्यान रखते हुए करते हैं। प्रायः माना जाता है कि ‘अनूदित पाठ’ ‘मूल पाठ’ के पूर्ण समतुल्य नहीं हो सकता। इसमें आंशिक रूप से कुछ कमी रह ही जाती है। साहित्यिक अनुवाद में यह समस्या अधिक होती है, साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक, शैलीगत स्तर पर भी हो सकती है। साहित्य में कुछ प्रसंग, संदर्भ एवं शब्द प्राय: सार गर्भित होते हैं। अनुवादक के लिए उनका पूर्ण रूप से अनुवाद करना अत्यंत कठिन होता है। प्रख्यात भाषाविद् रवींद्रनाथ श्रीवास्तव समतुल्यता के सिद्धांत के आधार पर दूसरी भाषा के संगठनात्मक रूपांतरण को अनुवाद स्वीकार करते हैं। “एक भाषा (स्रोत भाषा) की पाठ सामग्री में अंतर्निहित तथ्य का समतुल्यता के सिद्धांत के आधार पर दूसरी भाषा (लक्ष्यभाषा) में संगठनात्मक रूपांतरण अथवा सर्जनात्मक पुनर्गठन को ही अनुवाद कहा जाता है।”5 अनुवादनीयता की समस्या के समाधान के लिए अनुवादक को चाहिए कि वह मूल पाठ के प्रत्येक पक्ष (भावगत, अर्थगत, संप्रेषणगत, व्याकरणगत एवं प्रयोजनगत) का अध्ययन करें जिससे प्रत्येक पक्ष का अधिक्तम अनुवाद हो सके एवं जिस पक्ष की अधिक्तम अनुवादनीयता हो, उसका उसी पक्ष पर अनुवाद करें।
बीसवीं शती में पाश्चात्य अनूदित साहित्य का विकास अभूतपूर्व रूप से हुआ है। न केवल साहित्य बल्कि दर्शन, विज्ञान, समाजशास्त्र इत्यादि सभी विषयों में अनुवादकार्य हो रहे हैं। वर्तमान समय में अनूदित साहित्य अत्यंत व्यापक और बहुआयामी है। यूरोप, अमरीका, जापान, चीन आदि देशों के अनुवादक न केवल अपने प्राचीन ग्रंथों बल्कि विश्वभर के महान साहित्य का भी अनुवाद कर रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों की सभ्यता एवं संस्कृति में अनेक भिन्नता देखने को मिलती है। इसलिए इन साहित्य एवं साहित्येत्तर रचनाओं का अनुवाद करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
अनुवाद करते समय अनुवादक को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें कुछ समस्या व्याकरणगत होती हैं, तो कुछ संस्कृतिगत। व्याकरणगत समस्या में अनुवादक के समक्ष संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि का अनुवाद करते समय अनेक समस्याएँ आती है। संज्ञा के संदर्भ में बात करें तो भिन्न सभ्यता एवं संस्कृति वाले स्थानों के व्यक्तियों के अनुवाद करने में समस्या आती है।
संज्ञा – संज्ञा का तात्पर्य नाम से है। यह नाम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, समूह, गुण अथवा भाव आदि का नाम हो सकता है। उदाहरण – सेब, शिवाय, भारत, नदी, पर्वत, राष्ट्रवाद, थकान आदि।
प्रत्येक समाज की भाषा, सभ्यता एवं संस्कृति में अपने शब्द होते हैं जिसके नाम अलग-अलग होते हैं। जिसका दूसरी भाषा में मिलना कठिन होता है।
संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद हैं –
- व्यक्तिवाचक संज्ञा – ऐसे शब्दजो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं।
जैसे – सुमन, कलम, जलेबी, जयपुर आदि।
- जाति वाचक संज्ञा – ऐसे शब्द जो किसी समूह/ जाति विशेष का बोध कराते हैं।
जैसे – नदी, पर्वत, भारतीय सेना, स्त्री-पुरुष आदि।
- भाव वाचक संज्ञा – ऐसे शब्द जो किसी गुण, भाव एवं धर्म के नाम का बोध कराते हैं।
जैसे – थकान, भूख, ईमानदारी आदि।
अपवाद – कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक दोनों संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
जैसे – गांधी, शास्त्री, नेताजी।
अपवाद – कुछ नाम किसी गुण के आधार पर रूढ़ कर दिये जाते हैं। साहित्य में इनका विशेष स्थान है।
जैसे – गधा (मूर्ख), बैल (परिश्रमी), उल्लू(मूर्ख), लोमड़ी(धूर्त) आदि।
साहित्य में पात्रों के संकेतार्थ नाम का महत्त्व – हिंदी साहित्य एवं भारतीय समाज में अनेक प्रकार के नाम देखने को मिलते हैं। साहित्यकार न केवल अपनी रचना के शीर्षक को संकेतार्थक रूप में प्रस्तुत करता है बल्कि अपने पात्रों के नाम भी संकेतार्थ रूप में रखता है। जिसमें समाज एवं साहित्य में अपने संकेतार्थ जिसमें लक्षणा अथवा व्यंजना को प्रस्तुत करते हैं। जिससे उस पत्र के नाम मात्र से उस पात्र के स्वभाव, उसके समाज की जानकारी, रचना की पृष्टभूमि आदि जानकारी देने का प्रयास करता है।
जैसे – मुंशी प्रेमचन्द द्वारा अपने उपन्यास ‘गोदान’ के पात्रों के नाम अपने वर्ग, समाज में स्थान को प्रदर्शित करता है। गोबर, होरी, धनिया, झुनिया, राय साहब, मिस्टर खन्ना आदि। ऐसे ही मोहन राकेश के आधे-अधूरे नाटक की पात्र का नाम सावित्री एक व्यंजनापरक नाम है।
अन्य रूप में देखे तो साहित्यकार समाज में प्रचलित अनेक लक्षणापरक एवं व्यंजनापरक नामों का प्रयोग करते हैं जो उनके गुणों के आधार पर रूढ़ हो गए हैं। जैसे – गधा – बिना दिमाग के काम करने वाला, बैल – परिश्रमी, श्रवण कुमार – आज्ञाकारी पुत्र, रामराज्य – आदर्श राज्य, सावित्री – आदर्श पत्नी, जल – पूजा में प्रयोग होने वाला पानी।
‘तेनाली राम’(विद्वान), ‘शेखचिल्ली’(मूर्ख व्यक्ति), ‘हातम ताई’ (उदार व्यक्ति)।
साहित्येत्तर विषयों में नाम का महत्त्व – साहित्येत्तर विषयों के अनुवाद की समस्या मुख्य रूप से विषय-क्षेत्र की समस्या होती है। ये अनुवाद विज्ञान, अनुसंधान आदि विषयों में हो सकते हैं। इनके अनुवाद में दूसरी भाषा के नाम से स्थानांतरण न कर मूल नाम का लिपयंतरण दूसरी भाषा में करना चाहिए। यदि किसी वस्तु अथवा नाम का अनुवाद करना हो तो उसके अर्थ को व्याख्यायित किया जा सकता है। जैसे – अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन(ILO) – International Labour Organisation. अंग्रेज़ी से अनुवाद करते समय यह समस्या अधिक देखने को मिलती है। जैसे – Iron Plant – लौह पौधा।
हिंदी समाज में मुख्य रूप से नाम के दो अंग देखने को मिलते हैं किन्तु कभी-कभी इसके तीन अंग भी देखने को मिलते हैं– प्रथम नाम, द्वितीय नाम, तृतीय नाम।
प्रथम नाम – यह नाम व्यक्ति का मुख्य वैयक्तिक नाम होता हैं।
जैसे – शिवाय, जॉन, अहमद, परमजीत आदि।
अनेक स्थान पर नाम से पूर्व अपने माता-पिता एवं स्थान के नाम के प्रथम वर्ण को लिखने का प्रचलन है। किन्तु हिंदी समाज में ऐसा प्रचलन देखने को नहीं मिलता।
मध्य नाम – यह नाम के मध्य का हिस्सा होता है जो मुख्य रूप से उनके गुण को प्रदर्शित करता है। तो कुछ स्थानों पर व्यक्ति के माता-पिता का नाम जुड़ा होता है। हिंदी समाज में इसकी प्रचलन अधिक पुराना नहीं है। यहाँ मुख्य रूप से प्रथम एवं अंतिम नाम का प्रचलन अधिक दिखायी पड़ता है।
जैसे – मोहनदास कर्मचन्द गांधी – यहाँ मध्य नाम कर्मचन्द इनके पिताजी का नाम है।
शानिध्य प्रताप गुर्जर – यहाँ प्रताप शौर्य के गुण को प्रदर्शित कर रहा है।
अंतिम नाम – ये नाम व्यक्ति की जाति, स्थान से जुड़े होते हैं।
जैसे – राहत इन्दौरी, साहिर लुधियानवी, प्रणव गुर्जर। यहाँ इन्दौरी एवं लुधियानवी क्रमश: इंदौर एवं लुधियाना शहर को दर्शाता है तो गुर्जर एक जाति का द्योतक है।
उपाधि नाम – ऐसे नाम जो किसी व्यक्ति को उसके गुण-धर्म एवं कार्य के आधार पर दिये जाते हैं। ये नाम इतने रूढ़ हो जाते हैं कि उसके असली नाम से भी अधिक प्रसिद्ध हो जाते हैं।
जैसे – लौहपुरुष एवं सरदार – वल्लभभाई पटेल , महात्मा – मोहनदास गांधी।
सामान्यत: ऐसा प्रचलन भी देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति का उपाधि नाम उसके परिवार द्वारा (उपनाम के रूप में) परंपरागत रूप में प्रयोग किया जाता है।
जैसे – राजेश पायलट (जो एक पायलट थे) उनके पुत्र एवं परिवार भी पायलट उपनाम का प्रयोग करता है।
उपनाम (Pen Name) – ये ऐसे उपनाम होते हैं जिसे मूल रूप से लेखक अथवा साहित्यकार अपने साहित्य के लिए चुनते हैं।
जैसे – सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’, सुमित्रा नंदन ‘पंत’, अवतार सिंह संधू ‘पाश’, सुदामा पांडे ‘धूमिल’।
उपनाम (Pet Name) – ये ऐसे उपनामहोते हैं जिसे प्रायः परिवार एवं मित्रों के द्वारा दिया जाता है।
जैसे – लड्डू, मिट्टू, कृष्णा।
पारिवारिक नाम – किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े कार्यों में भी उनके अपने परिवार, कुटुंब आदि रूप में देखे जाते हैं। जैसे – शास्त्रीय संगीत की घराना परंपरा, व्यापारिक परिवार आदि।
मातृक नाम – ये ऐसे नाम है जो व्यक्ति को अपनी मातृ पक्ष से मिलता है।उत्तर भारत अथवा हिंदी समाज में मुख्य रूप से पितृसत्तमक समाज है, यहाँ मातृ पक्ष का नाम जोड़ने का प्रचलन नहीं मिलता। किन्तु इतिहास में देखे तो रामायण एवं महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है।
जैसे – मुग़ल अपने मातृ पक्ष से मंगोल थे, सुमित्रानंदन – लक्ष्मण, कुंतीपुत्र – अर्जुन।
पैतृक नाम – ये ऐसे नाम है जो व्यक्ति को अपने पितृ पक्ष से मिलता है।
जैसे –राहुल गांधी – राजीव गांधी,मुग़ल अपने पितृ पक्ष से तैमूर वंशी थे।
स्त्रीसूचक नामक – कुछ ऐसे नाम, उपनाम होते हैं जो केवल स्त्रियोचित्त होते हैं।
जैसे – जननी, सुलक्षणा, सीता, देवी, कौर।
परंपरागत नाम – ऐसे नाम जो व्यक्ति की परंपरा से जुड़े रहते हैं। हिंदी समाज में ऐसे नाम का प्रचलन कम मिलता है। यूरोप एवं मुगल राजशाही परिवारों में इसका प्रचलन देखने को मिलता है।
मुगल – अकबर, अकबर द्वितीय।
यूरोप – किंग चार्ल्स, किंग चार्ल्स द्वितीय, किंग चार्ल्स तृतीय।
विद्वानों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा के अनुवाद के संबंध में विभिन्न विचार प्रस्तुत किए हैं।
पीटर न्युमार्क – इनका मानना है कि व्यक्तियों के नाम उनके संकेतार्थ के साथ अनूदित कर देने चाहिए।
साथ ही कल्पनात्मक साहित्य के ऐसे नाम जिनका संकेतार्थ से जुड़े हों उनका लक्ष्य भाषा में उचित शब्द से स्थानांतरित करना उचित होता है।6
थियो हरमन – इन्होंने मूल नाम का अनुवाद करने के चार आधार हैं –
- उसे लक्ष्य भाषा के साथ मूल भाषा में हूबहू लिखा जाना चाहिए।
- उसका लक्ष्य भाषा में लिपियंतरण किया जा सकता है। यद्यपि हिंदी से अनुवाद करते समय इस प्रकार की समस्या नहीं आती। अंग्रेज़ी के ‘silent alphabet’ में इसकी समस्या आ सकती है। जैसे – Knife – नाईफ ।
- यदि मूल नाम को स्थानांतरित किया जा सकता है तो उसे लक्ष्य भाषा के किसी भी अन्य नाम से स्थानतारित कर दिया जाए।
- मूल नाम को लक्ष्य भाषा के किसी ऐसे नाम से स्थानतारित किया जाए जो उसके समान अर्थ रखता हो। साथ ही मूल नाम का अर्थ भी वर्णित कर देना चाहिए।7
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ‘Plain Living High Thinking’ का ‘आदर्श जीवन’ नामक अनूदित पुस्तक के रूप में अनुवाद करते हुए लिखते हैं – “जहाँ-जहाँ अंग्रेज़ी पुस्तक में दृष्टांत रूप में योरप के प्रसिद्ध पुरुषों के वृतांत आए हैं, वहाँ- वहाँ यथा संभव भारतीय पुरुषों के दृष्टांत दिए गए हैं।”8
संज्ञा का अनुवाद करने के लिए अनुवादक को मूल रचना एवं अनूदित रचना दोनों की भाषा, संस्कृति का उत्तम ज्ञान एवं समझ होनी आवश्यक है। जिससे वह संज्ञा में छिपे गूढ़ अर्थों जैसे लिंग, धर्म-संप्रदाय, जाति, क्षेत्र, गुण एवं भाव आदि को जान सके एवं मूल रचना एवं रचनाकार के साथ-साथ पाठक के साथ न्याय कर सके। जिससे वह ‘मूल भाषा’ के शब्द के लिए ‘लक्ष्य भाषा’ के सर्वोत्तम शब्द का चुनाव कर सके।
इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का अनुवाद करना अनुवादक के लिए एक गहरी चुनौती का कार्य है। जिसके लिए अनुवादकों ने विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किये हैं। कुछ विद्वान संज्ञा के अनुवाद के लिए लिप्यंतरण, रूपांतरण करने की सलाह देते है तो कुछ लक्ष्य भाषा के शब्द से इसे स्थानांतरित करने की सलाह देते हैं। इनमें से किसी भी शैली को एक आदर्श तरीका नहीं माना जा सकता। ये शैली मूल रचना के विषय-क्षेत्र, अनुवादक के अनुवाद के उद्देश्य, अनूदित रचना के पाठक वर्ग आदि सभी तत्वों पर निर्भर करते हैं।
ऐसे कुछ सुझाव हैं जिसके आधार पर इस चुनौती को कुछ स्तर तक सरल किया जा सकता है –
- अनुवादक को चाहिए कि संप्रेषण की सुगमता के लिए कोष्टक में मूल नाम को भी साथ में लिख दे। यद्यपि इससे पढ़ने के तारतम्य में कुछ बाधा उत्पन्न हो किन्तु विषय की बोधगम्यता के लिए यह सहायक है।
- अनुवादक को चाहिए कि मूल नाम एवं उससे संबंधित जानकारी को फुटनोट अथवा अंत में लिख दे। यदि ‘मूल भाषा’ के नाम का लगभग समान पर्याय वाला नाम ‘लक्ष्य भाषा’ में प्राप्त होता हो तो उसे अवश्य अपनाना चाहिए।
- अनुवाद करते समय अनुवादक को ‘मूल नाम’ के समान लिए ‘समान अथवा लगभग समान नाम’ (व्यक्ति का नाम) उपलब्ध न हो पाए तो अनुवादक को अनुवाद की सुगमता के लिए ‘मूल नाम’ का प्रयोग अनुवाद करना चाहिए। साथ ही पाठक वर्ग की सहुलियत के लिये ‘पाद टिप्पणी’ में शब्द के सांस्कृतिक संदर्भ, उसकी परंपरा तथा नाम विषयक विशेषता को स्पष्ट कर दे। ‘मूल नाम’ के सांस्कृतिक संदर्भ, विशिष्ट विधि विधान, परंपराएं, आचार विचार, खान-पान, वेशभूषा, पूजा-पाठ, व्रत उपवास, रिश्ते-नाते विवाह, संस्कार आदि से संबंधित समान शब्दावली न मिलने पर तद्विषयक यथोचित स्पष्टीकरण, जानकारी एवं आवश्यक सामग्री को सूची परिशिष्ट में दे।
- अन्य स्थिति जिसमें ‘मूल भाषा’ के किसी शब्द, संकल्पना, वस्तु या कार्य के लिए ‘लक्ष्य भाषा’ में न केवल पर्याय शब्द देकर बल्कि स्पष्टीकरण द्वारा समझाने का प्रयास करना चाहिए। तब भी बात न बने, तो परिशिष्ट में तत्संबंधी शब्द, वस्तु अथवा नाम का चित्र के माध्यम से संप्रेषण को सुगम बनाया जा सकता है। मुख्य रूप से वेशभूषा, गहने, खाद्य सामग्री, विधि-विधान, दैनदिनी जीवन के अवयव, विविध सांस्कृतिक संदर्भ, वस्तुएँ आदि का चित्र द्वारा लक्ष्य भाषा में दर्शाया जा सकता है।
- अनुवाद कार्य में सुगमता लाने के लिए ‘सांस्कृतिक कोश’ का उपयोग किया जाना चाहिए। जिससे ‘मूल भाषा’ के सांस्कृतिक शब्दों के समान ‘लक्ष्य भाषा’ में उसका प्रतीकात्मक नाम ढूँढा जा सके। बहुभाषी ‘सांस्कृति कोश’ का उपयोग अनुवाद की सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने का एक बेहतर उपाय हो सकता है।
निष्कर्ष – इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा मुख्य रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा का अनुवाद करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जिसके लिए अनुवादक को मूल एवं लक्ष्य दोनों भाषाओं के शब्द-भंडार, व्याकरण एवं संस्कृति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जिससे मूल रचना के विषय के आधार पर कभी मूल नाम तो कभी समान एवं लगभग समान नाम प्रयोग कर अनुवाद को प्रभावी बनाया जा सकता है। जिससे मूल रचना, रचनाकार एवं अनूदित पाठ के पाठकवर्ग के साथ न्याय हो सके।
संदर्भ सूची
- अनुवाद चिंतन, प्रोफेसर अर्जुन चौहान, अमन प्रकाशन, द्वितीय संस्करण-2020 , पृष्ठ सं० 47
- अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि, भोलानाथ तिवारी, किताबघर प्रकाशन, संस्करण-2016, पृष्ठ सं० 15
- अनुवाद की नई परंपरा और आयाम, कृष्ण कुमार गोस्वामी, प्रकाशन संस्थान, संस्करण-2016, पृष्ठ सं० 15
- वही, पृष्ठ स० 19
- अनुवाद विज्ञान सिद्धांत और प्रयोग, कैलाश चंद्र भाटिया, तक्षशिला प्रकाशन, संस्करण – 5, पृष्ठ स० 3
- Approach to Translation, Peter Newmark, phoenix elt publisher, page no 214
A Textbook of Translation, Peter Newmark, phoenix elt publisher, Page no 151
7. Nord, C. (2003), Proper Names in Translation for children: Alice in Wonderland as a case of Point. Meta: Translators’ journal, 48, 182-196.
8. आचार्य रामचंद्र शुक्ल ग्रंथावली, सं० नामवर सिंह, खंड-7, पृष्ठ स 325,
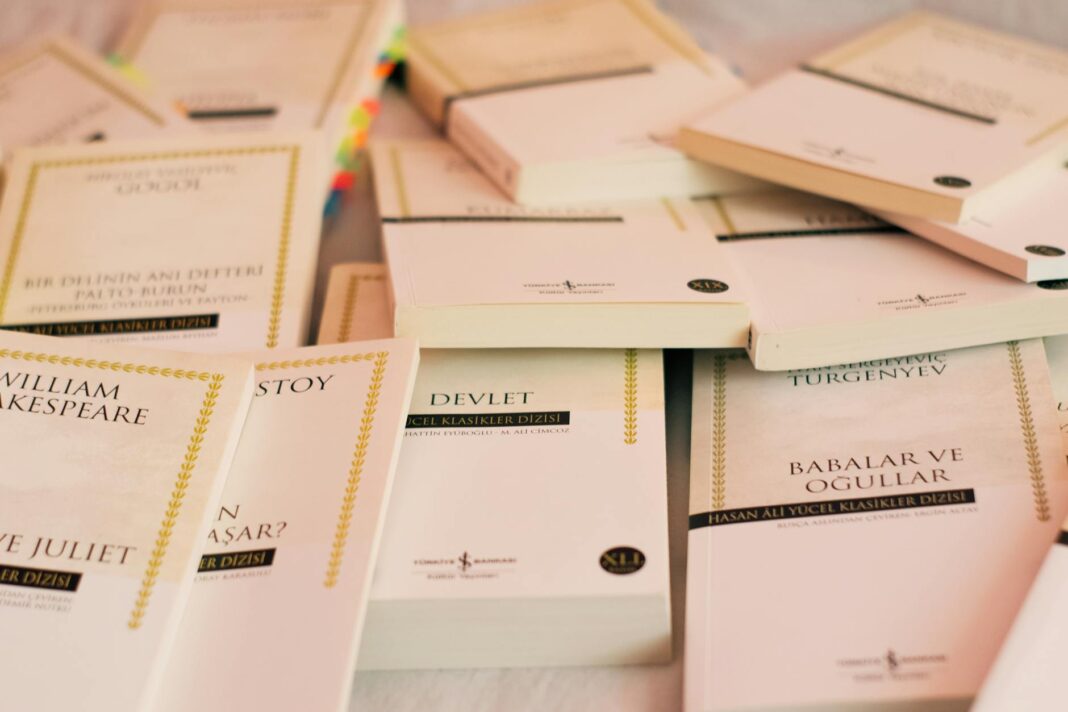

![असम का सांस्कृतिक पर्यटन : अनुवाद और निर्वचन की वर्तमान स्थिति एवं समस्याएँ-उज्जवल डेका बरुआ hills covered with green plants ]](/wp-content/uploads/2021/02/ravi-pinisetti-ysqxozlasmc-unsplash-scaled.jpeg)