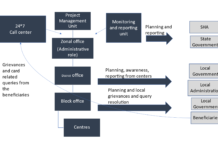आवां : विकलांगता और उसका प्रभाव
डॉ. संध्या कुमारी पीएचडी जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 9818799240 sandhyajnu76@gmail.com
सारांश (Abstract) :
सुप्रसिद्ध लेखिका चित्रा मुद्गल का आवां उपन्यास समाज के इस तबके में स्त्री की स्थिति और उसके शोषण के विभिन्न स्तरों को उजागर करता है कामगार अघाड़ी के महासचिव देवीशंकर पांडेय की बेटी नमिता के जीवन संघर्ष के साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों के स्त्रियों का जीवन संघर्ष इस उपन्यास की कथानक के रेशे-रेशे में मौजूद है | नमिता के संघर्ष का मुख्य कारण उसकी पिता की विकलांगता से उत्पन्न परिस्थितियाँ हैं | किसी भी परिवार में जब कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता है तो उसका प्रभाव परिवार के सभी सदस्यों के जीवन पर पड़ता है | स्त्री-पुरुष दोनों का ही सफल गृहस्थी में समान महत्त्व होता है | नमिता की माँ अपने दायित्वों को निभाने में असफल रहती है जिसका प्रभाव नमिता की पढ़ाई पर पड़ता है |
बीज शब्द (Keywords)– आवां, विकलांगता, परिस्थितियाँ, संघर्ष, आत्मविश्वास, देखभाल,
भूमिका (Introduction)
सुप्रसिद्ध लेखिका चित्रा मुदगल का ‘आवां’ उपन्यास समाज के हर तबके में स्त्री की स्थिति और उसके शोषण के स्वरूप को उजागर करता है। यह समाज में व्याप्त विसंगतियों, उसके पाखंड और कुरीतियों को अभिव्यक्त करता है। इसके माध्यम से लेखिका दिहाड़ी पर जी रहे मजदूरों, श्रमिक वस्तियों के नग्न यथार्थ मजदूर नेताओं के अन्तर्विरोध, वेश्या जीवन एवं उनके पुनर्वास के प्रयास एवं समस्या तथा जाति और धर्म के आधार पर अपनी रोटी सेंकने वाले धर्म के ठेकेदारों को बेनकाब करने का सफल प्रयास किया है। नामवर सिंह के अनुसार ‘आवां’ उपन्यास उस वर्ष का ही नहीं, उस दशक का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है।1
शोध आलेख
इस उपन्यास के केन्द्र में है नमिता। नमिता के पिता देवीशंकर पांडेय ‘कामगार आघाड़ी’ के महासचिव हैं। श्रमिक आंदोलन के दौरान ही कोई भीतरघाती उनके पीठ में छुरा भोंक देता है। उनकी जान बच जाती है। जिन्दगी में कर्म को प्रधान मानने वाले तथा कामगार आघाड़ी के प्रति समर्पित नमिता के पिता चलने-फिरने के लायक होते ही आघाड़ी के कार्यालय में बैठना शुरू कर देते हैं, जिसका दुष्परिणाम उन्हें ही नहीं उनके परिवार वालों को भी झेलना पड़ता है। ‘जर्जर देह-दिमाग-सार्मथ्य से अधिक परिश्रम एवं तनाव नहीं झेल पाया। आघाड़ी कार्यालय में ही एक सांझ अस्थायी श्रमिकों के हित-संघर्ष की रणनीति बनाते हुए लकवा ग्रस्त हो गए। 2
हालाकि देवीशंकर पांडेय का विकलांगता से ग्रस्त होते ही नमिता के जीवन में समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ता है। नमिता के जीवन की विसंगतियों, बिडम्बनाओं, शोषण एवं अभावग्रस्त जीवन के पीछे कहीं-न-कहीं उसके पिता की विकलांगता की समस्या ही मुख्य है। लेखिका का उद्देश्य विकलांग जीवन की समस्याओं को दिखाना नहीं है पर नमिता के जीवन की तमाम घटनायें उसके परिवार से भी तो जुड़ी हुई है। परिवार की धूरी बाबूजी के विकलांग होने से उसकी पढ़ाई छूट जाती है। यहाँ समस्या सिर्फ आर्थिक ही नहीं है। समस्या बाबूजी की परिचर्या की भी है। नमिता जैसी साहसी लड़की साड़ियों में फाल टाक कर, ट्यूशन पढ़ाकर, पापड़ बेलकर किसी तरह अपने पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ ही लेती।
परिवार के सम्यक संचालन में जितना महत्त्व एक पुरूष का होता है उतना ही एक औरत का। पति के लकवाग्रस्त होने के पश्चात् यदि नमिता की माँ घर में अपने बुजुर्ग होने के दायित्व को संभाल पातीं तो नमिता का जीवन इस तरह न बिखरता। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पति की सेवा बिल्कुल नहीं की। कुछ दिनों तक तो माँ ने भी देखभाल में कोई कोर-कसर नहीं बरती लेकिन जल्दी ही वे परिचर्या की एकरसता से ऊबकर दायित्व उसे सौंप किनारे होलीं। नमिता की माँ में देखभाल के लिए आवश्यक धैर्य का अभाव है। वह अक्सर नमिता को तानें देने लगती हैं – ‘‘कहाँ-कहाँ मरूँ और क्या-क्या करूँ? जिसे देखो कलेक्टर बनने में अधिया रहा। मूड़ने को बच गई मैं अनपढ़ गंवार … जरखरीदी बाँदी।’’3 अपने माँ की कटोक्तियों से परेशान नमिता अपने पिता की परिचर्या का भार उठा लेती है। उसमें उसका हाथ बँटाती है छोटी बहन मुनिया। यदि उसकी माँ पति की सेवा में कोताही न बरतती तो नमिता की पढ़ाई न छुटती। पढ़ाई छूटने की टीस से नमिता सदैव परेशान होती है। पढ़ाई छूटने और एक साल व्यर्थ गवाँ देने का दुख उसे भीतर ही भीतर दीमक की तरह खोखला कर रहा है।
नमिता के अपनी माँ का व्यवहार बिल्कुल अजीब लगता है। नमिता और उसकी माँ के संबंधों के माध्यम से लेखिका ने एक स्त्री के मन में दूसरी स्त्री प्रति छिपे ईष्र्या के भाव को उजागर किया है। यहाँ नमिता और उसकी माँ के संबंध माँ-बेटी की तरह स्नेहिल एवं ममतापूर्ण नहीं है। नमिता की माँ नमिता को अपने बरक्स एक दूसरी स्त्री के रूप में देख रही है। यही कारण है कि वह उससे अनजाने ही ईर्ष्याभाव रखने लगी है। जो उसे न मिला वह किसी भी कीमत पर नमिता को भी नहीं पाने देना चाहती। इसी तरह का ईर्ष्याभाव या मनोवृतिया हमें मनु भंडारी की कहानी ‘असमर्थ हिलाता हाथ’ में द्रष्टव्य होता है। नमिता का सोचना बिल्कुल सही है कि यदि माँ चाहती तो अपने कुछ आभूषणों को बेचकर नमिता की पढ़ाई जारी रख सकती थीं। पर उसे नमिता के बेहतर भविष्य की कोई परवाह ही नहीं। उन्हें नमिता के हर कार्यकलाप को संदिग्ध दृष्टि से देखती है। चाहे उसका रोजगार कार्यालय जाना हो या कोई अन्य कार्य। नमिता को जलील करने के लिए वह नये-नये हथकंडे अपनाती है।
इस तरह स्पष्ट है कि परिवार में कोई एक व्यक्ति विकलांग हो जाता है तो उससे जुड़ी तमाम जिन्दगियाँ प्रभावित होती हैं। उसके सेवा-सुश्रुषा को लेकर भी अक्सर परिवार में तनाव का माहौल होता है। कम ही ऐसे परिवार होते हैं जहाँ इसे चुनौती की तरह स्वीकार किया जाता है और विकलांग व्यक्ति की परिचर्या सहज रूप से होता है। ‘आवां’ में देखभाल की समस्या को लेकर नमिता परेशान रहती है। नौकरी छूटने पर भय का सर्वोपरि कारण हैं बिस्तर से लगे बाबूजी के खाने-पीने की! ट्टी-पेशाब करवाने की।
भिन्न-भिन्न आर्थिक परिस्थिति के अनुसार समाज और परिवार में विकलांगों की स्थिति भी भिन्न-भिन्न होती है। उनकी समस्याएँ अलग होती हैं। यदि नमिता के पिता की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती तो न तो परिचर्या की समस्या नमिता के सामने आती और न ही नौकरी ढ़ूँढ़ने की। उसकी पढ़ाई सुचारू ढ़ंग से चलती और विकलांग पिता की सेवा-सुश्रुषा के लिए वह किसी को नौकरी भी दे सकती थी। ‘‘बाबूजी स्वस्थ होते तो क्या उसकी सांध्यकालीन कक्षाओं में दाखिला लेने की नौबत आती? चैथे माले वाली ममता की भाँति ऐंठ से दोहरी होती हुई, पेंसिल एड़ियां सीढ़ियों पर ठकठकाती कालेज न जा रही होती?’’4
नमिता मैडम वासवानी से कह तो देती है कि पिता स्वस्थ होते तो उसके लिए सांध्यकालीन कक्षाओं में नामांकन हेतु प्रयास करते पर उसे अपनी ही बातों के खोखलापन का अहसास होता है कि यदि पिता स्वस्थ होते तो उसे सांध्यकालीन कक्षाएँ लेने की जरूरत ही नहीं होती। मैडम वासवानी जैसी काइयां औरत मदद करके उसका विश्वास अर्जित कर लेती हैं। घबराई और असंयत नमिता एवं इंटरव्यू देती नमिता से बड़ी चतुराई से उसके घर परिवार की सारी स्थितियाँ जान लेती है कि नमिता की केवल आर्थिक हो नहीं पारिवारिक स्थिति भी जर्जर है। उसके सिर पर किसी बड़े व्यक्ति का हाथ नहीं। वह नमिता से उसके अन्ना साहब के यहाँ नौकरी छोड़ने का कारण भी जान लेती है।
जब कोई व्यक्ति विकलांगता से ग्रस्त होता है तो उसका स्वयं का जीवन तो मुश्किल होता ही है, उसके परिवार वालों की भी दिनचर्या स्वाभाविक नहीं रह पाती। इसकी प्रतिक्रिया समाज में दो तरह से देखने को मिलती है। कुछ परिवारों में या कुछ लोगों में विकलांग व्यक्ति प्रमुख होता है। उसको जीवित रखना, उसे सकारात्मक वातावरण देना प्रमुख रहता है। इसके लिए चाहे जो भी कष्ट झेलने पड़े। जैसे नमिता बाबूजी को अस्पताल जाने पर सोचती है ‘‘जिस हालात में भी रहे बाबूजी, उनके बीच बने रहें। जिम्मेदारियाँ ढ़ो लेगी वह अकेली। कोर-कसर नहीं छोड़ेगीं सेवा में।’’5
नमिता के लिए महत्त्वपूर्ण हैं बाबूजी का साथ। उनकी सेवा-सुश्रुषा, इलाज आदि के क्रम में होने वाली परेशानियाँ बाबूजी के सान्निध्य के सामने महत्त्वहीन है। वह हर हालत में बाबूजी को जीवित देखना चाहती है, क्योंकि बाबूजी से उसे चारित्रिक सबलता, मनोबल, दृढ़ता अन्याय के विरोध की प्रेरणा, विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता मिलती है। वह अपनी शंकाओं का समाधान बाबूजी से करवाती है। बाबूजी स्लेट पर लिख अपने बच्चों से सहज बातचीत ही नहीं करते बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। जबकि पूरी तरह से स्वस्थ माँ बीमार मानसिकता का उदाहरण है जिसके लिए लड़कियों का होना-न-होना बराबर है। परिवार के भविष्य के रूप में, बुढ़ापे के सहारे के रूप में उसकी एकमात्र आशाएँ बेटे से बँधी है। नमिता का त्याग, मेहनत, परिवार के लिए कुछ कर गुजरने की भावनाएँ उसे नहीं दिखतीं। अपनी बहन कुंती के बेटे-बेटियों में उसे हजार गुण नजर आते हैं पर अपने बेटियों का गुण भी उसे दोष ही लगता है। माँ के अत्याचार और दमन के विरोध में जहाँ नमिता में विद्रोह की भावना पनपती हैं वहीं पुनियाँ में आत्महत्या की भावना। निरपराध पुनियाँ की पिटाई से तिक्त हो गई नमिता का दिल करता है कि उसी तरह उनकी भी पिटाई कर दे पर माँ का पद ही उनकी रक्षा कवच बन जाता है। बैठक की दीवान पर असहाय पड़े बाबूजी का ख्याल कर वह चुप रह जाती है। जिस बाबूजी की नींद माँ के चीखने-चिल्लाने से भी नहीं खुलती वही नमिता की तेज आवाज पर चिहुँककर आँखें खोल देते और अस्पष्ट रिरियाहट से उसे पुकारते हुए नाना सवाल करते है |
नमिता के बाबूजी विकलांगता के पूर्व जिस प्रकार के कर्मठ, आत्मविश्वासी और जीवट थे विकलांगता के बाद उसमें कोई कमी नहीं आयी थी। वह अक्सर अपने बच्चों से कहते हैं – ‘आत्मविश्वास हर संकट की कुंजी है।’6 कभी स्लेट पर लिखते हैं – ‘जिस व्यक्ति में आक्रोश नहीं वह अनीति से नहीं लड़ सकता।’7 नमिता के द्वारा कामगार अघाड़ी की नौकरी छोड़ने के निर्णय पर बाबूजी न तो घबराते हैं न उससे कोई सवाल करते हैं। बल्कि उसके स्वतंत्र निर्णय लेने की सराहना करते हैं- ‘‘मुझे खुशी है कि तुमने पहली बार अपने विषय में स्वतंत्र निर्णय लिया। विवेक जाग्रत है तुम्हारा, जाग्रत ही रखना। मैं तुझसे हरगिज नहीं पूछँगा कि तुम वहाँ नौकरी क्यों नहीं करना चाहती। निश्चिन्त होकर सो जाओ – नये भोर की प्रतीक्षा में, जिसे कोई सूत्र नहीं, स्वयं आदमी गढ़ता है।’’8
नमिता के पिता विवेकशील है जबकि उसकी तथाकथित सकलांग माँ बीमार मानसिकता से ग्रसित हैं। वह माँ का हर जुल्म सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर लेती है कि बाबूजी को घर के क्लेश से कोई मानसिक पीड़ा न हो। यह बंधन यानी बाबूजी जब नहीं रहे तो नमिता के लिए उस घर में रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता।
नमिता की माँ अपने पति की विकलांगता के कारण उनकी सेवा सुश्रुषा से जल्दी ही उब जाती है। उनके लिए पति का महत्व पहले भी न था। पर विकलांगता के बाद उसके लिए देवीशंकर पाण्डेय वैसे ही हो गए जैसे घर में पड़ा हुआ कोई सामान। उसे पति की मृत्यु का भी कुछ खास दुख नहीं होता। वह अपने पति की विकलांगता का यदा-कदा मजाक भी उड़ाती है। वह नमिता से कहती है – ‘‘अन्ना साहब को देखते ही तेरे बाबूजी के चेहरे मुर्दनी सूप की पहली फटक दी उड़े भूये सी इ हो गई। जो हमारे हजार फटके चुटकी भर भी उड़के नहीं देती, छौवी। बौराए से कौवा उठे कदम।’’9
माँ की ऐसी टिप्पणी पर नमिता को आश्चर्य होता है अपनी माँ के बातों और व्यवहार पर। उसका मन तिक्त हो उठता है। उसे आश्चर्य होता है कि कोई पत्नी अपने पति की अपंगता पर इतने सहज ढ़ंग से कैसे चटखारे ले सकती है।
इस उपन्यास से यह भी स्पष्ट होता है कि आर्थिक अभाव में विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति और उसके परिवार वाले कई बार न चाहते हुए भी नीम हकीम या अंधविश्वास की ओर चले जाते हैं। नमिता के पास किसी न्यूरोफिजिशियन को देने के लिए फी नहीं है इसलिए ऐसी हालत में हकीम मुन्ने मियाँ के द्वारा दिए गए तेल से बाबूजी के निर्जीव अंगों की मालिश करना ही एकमात्र सहारा है।
इस उपन्यास में यह भी दिखाया गया है कि किसी भी संस्था के लिए जीवन भर समर्पित व्यक्ति विकलांगता से ग्रसित होते ही कैसे किसी काम का नहीं रह जाता। उसकी सेवा, समर्पन, त्याग का कहीं भी सही मूल्यांकन नहीं हो पाता।
निष्कर्ष (Conclusion) :
आवां उपन्यासके माध्यम से स्पष्ट है कि किस तरह परिवार में किसी सदस्य के विकलांग होने से परिवार का आर्थिक ढाँचा चरमरा जाता है| खास तब तो और अधिक विकट हो जाता है जब परिवार का एकमात्र कमाने वाला ही विकलांगता के चपेट में आ जाय | इस चुनौती का यदि परिवार के सदस्यों द्वारा सौहार्द्धतापूर्ण तरीके से सामना न किया जाय तो उन सबके न केवल आर्थिक बल्कि अन्य क्षेत्र भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहता | कुटिल और धूर्त लोग उनकी इस परिस्थिति का नाजायज फायदा उठाने से बाज नहीं आतें | विकलांगता के बावजूद भी व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास हो तो वह दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत बं जाता है न कि पीड़ा दायक | देवीशंकर पांडेय की कर्मठता और जीवटता प्रणम्य है |
संदर्भ (Reference) :
1 करुणाशंकर उपाध्याय, आवां विमर्श, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2010, पृ. सं. 9
2 चित्रा मुदगल, आवां, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2014, पृ. सं. 69
3 वही, पृ. सं. 25
4 वही, पृ. सं. 21
5 वही, पृ. सं. 328
6 वही, पृ. सं. 225
7 वही, पृ. सं. 239
8 वही, पृ. सं. 143
9 वही, पृ. सं. 296