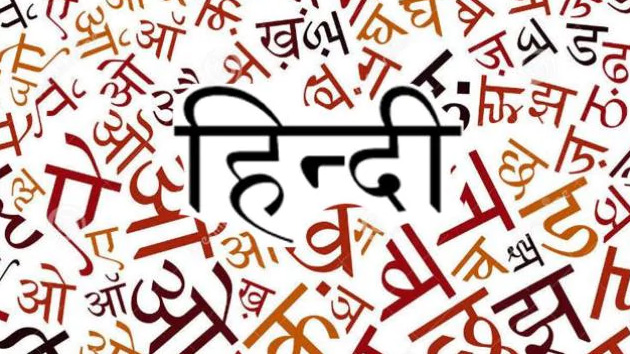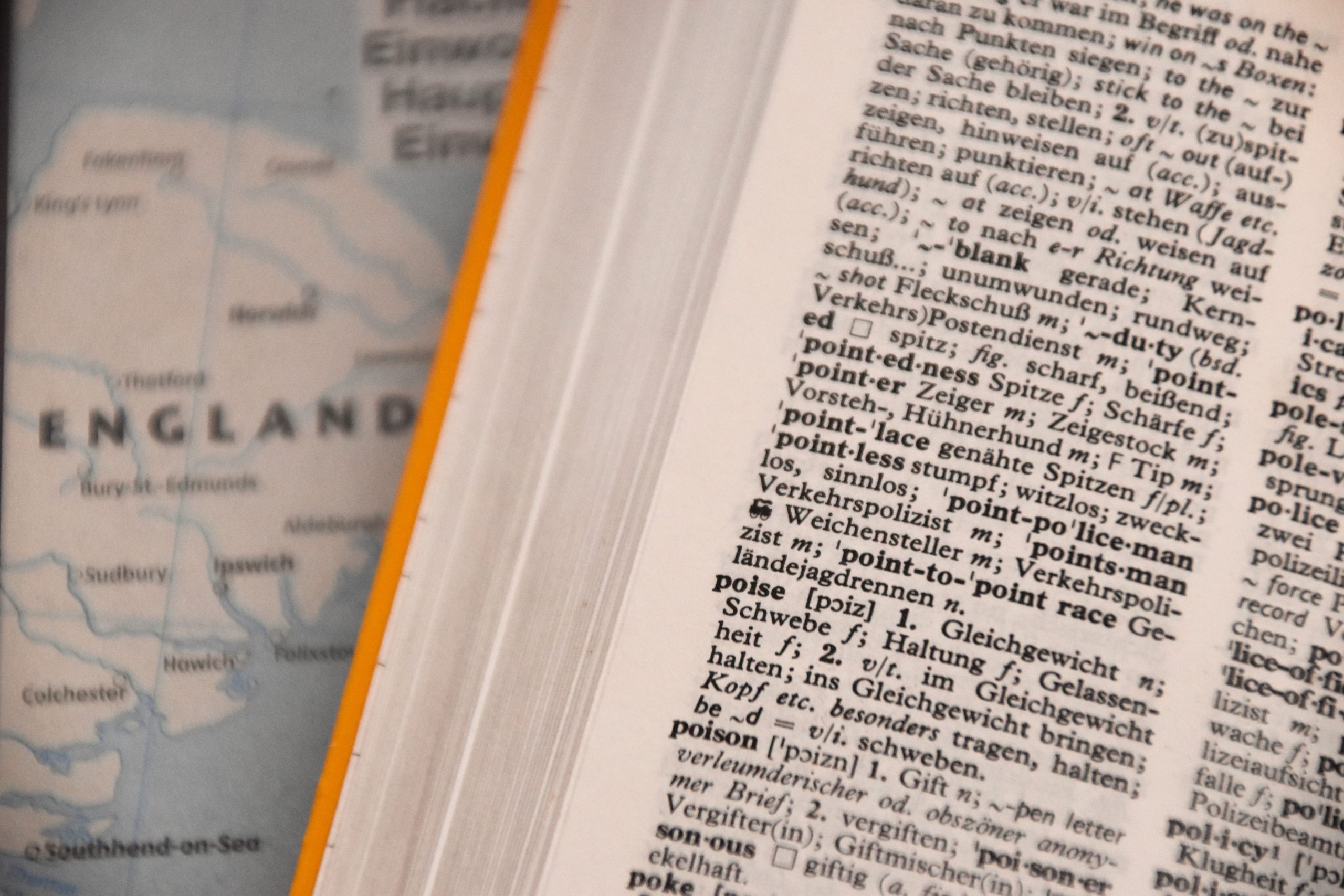स्वाधीन भारत में हिंदी का विस्तार
श्रीमती श्वेता सिंघल,
आई.एस.एस. सचिव राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य
शोधार्थी,हिंदी विभाग, मुंबई विश्वविद्यालय
सारांश
जब हम भाषा के क्रमिक विकास पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि कोई भी भाषा प्रारंभ में केवल बोलचाल की भाषा होती है। धीरे धीरे लोक परम्परा की अभिव्यक्ति का माध्यम जाती है। यह लोकगीतों, लोकनाटकों, नुक्कड नाटकों में मनुष्य व समाज की हार्दिक इच्छाओं का उनकी आप बीती के दर्द को अभिव्यक्ति का उनके लोक विश्वास का, समाज के उत्साह व उमंग का, उनकी खुशी उनके उत्साह का ‘लोकभाषा’ के रुप मे अभिव्यक्ति व संप्रेषण माध्यम बन जाती है।जैसे ही भाषा लिपिबद्ध होने लगती है तो धीरे–धीरे व्यक्तिगत पत्र व्यवहार में प्रयुक्त होने लगती है।वह पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक चेतना की अभिवाहिका का काम करती है। जैसे–जैसे यह भाषा व्यापक होने लगती है और अधिक परिष्कृत व परिमार्जित होने लगती है। तो उत्तम साहित्यिक रचना की संस्थात्मक पीठिका बन जाती है।फलस्वरूप उसके लिए साहित्यिक भाषा का आयाम भी खुल जाता है। अभी तक के अपने विमर्श में हमने पाया कि हिन्दीं में लोक साहित्य व परिनिष्ठित साहित्य की विकसित परम्परा आजादी के पहले ही प्रबल हो चुकी थी। साथ ही विदेशों में पत्र- व्यवहार के रुप में प्रयुक्त होने के कुछ दृष्टांत हमें प्राप्त होते हैं।
बीज शब्द: भाषा, विकास, लिपि, परंपरा, अभिव्यक्ति
शोध आलेख
जब हम भाषा के क्रमिक विकास पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि कोई भी भाषा प्रारंभ में केवल बोलचाल की भाषा होती है। धीरे धीरे लोक परम्परा की अभिव्यक्ति का माध्यम जाती है। यह लोकगीतों, लोकनाटकों, नुक्कड नाटकों में मनुष्य व समाज की हार्दिक इच्छाओं का उनकी आप बीती के दर्द को अभिव्यक्ति का उनके लोक विश्वास का, समाज के उत्साह व उमंग का, उनकी खुशी उनके उत्साह का ‘लोकभाषा’ के रुप मे अभिव्यक्ति व संप्रेषण माध्यम बन जाती है।जैसे ही भाषा लिपिबद्ध होने लगती है तो धीरे-धीरे व्यक्तिगत पत्र व्यवहार में प्रयुक्त होने लगती है।वह पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक चेतना की अभिवाहिका का काम करती है।
जैसे-जैसे यह भाषा व्यापक होने लगती है और अधिक परिष्कृत व परिमार्जित होने लगती है। तो उत्तम साहित्यिक रचना की संस्थात्मक पीठिका बन जाती है।फलस्वरूप उसके लिए साहित्यिक भाषा का आयाम भी खुल जाता है।
अभी तक के अपने विमर्श में हमने पाया कि हिन्दीं में लोक साहित्य व परिनिष्ठित साहित्य की विकसित परम्परा आजादी के पहले ही प्रबल हो चुकी थी। साथ ही विदेशों में पत्र- व्यवहार के रुप में प्रयुक्त होने के कुछ दृष्टांत हमें प्राप्त होते हैं।
वैसे तो भारत 15 अगस्त को अनगिनत संघर्षों के बाद 1947 को स्वतन्त्र हो गया था परन्तु स्वाधीन भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस समय से हिंदी के का प्रयास संस्थागत रूप में होने लगा जिसका अनवरत विस्तार होता रहा है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद भी अनेक प्रकार के संशोधनों और परिमार्जन से होकर यह भाषा अत्यंत परिमार्जित और अभिव्यक्तात्मक हो गई है। राजभाषा बनने के बाद हिंदी जीवन और जगत के अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त होने लगी। इसी बीच केंद्र सरकार ने हिंदी सलाहकार समिति, राजभाषा कायार्न्वयन समिति, राष्ट्रपति के आदेश, संसदीय भाषा समिति जैसे वैधानिक माध्यमों द्वारा राजभाषा हिंदी को आगे बढाया और आज स्थिति यह है कि हिंदी लगातार विकसित और विस्तारित हो रही है। आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के जमाने में विदेशों में हिंदी का महत्व बढ़ रहा है। भारत की प्रगतिशील अर्थव्यवस्था ने विश्व में हिंदी का आकर्षण बढ़ाया है| विदेशों में हिंदी शिक्षण पर अधिक बल दिया जा रहा है तथा प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक हिंदी का अध्ययन -अध्यापन हो रहा है।यह प्रशासनिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सभी प्रकार की उच्च कोटि में अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन गया है। वर्तमान समय में भारतीय प्रैद्योगिकीय संस्थान के शोध छात्र अपना शोध प्रबंध भी हिंदी में प्रस्तुत कर रहें हैं।
हिंदी भाषा के विकास में हिंदी सिनेमा का भी विशेष योगदान है| हिंदी अध्यापन के लिए भी, सिनेमा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है तथा कई विदेशी ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा देखकर हिंदी सीखी है। कुछ लोग भारतीय संस्कृति को करीब से जानने के लिए हिंदी सीखते हैं| कुछ व्यापारिक आवश्यकताओं के कारण और कुछ ऐसे भी है जिनका भाषाओं के प्रति लगाव उन्हें हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करता है।
मध्यकाल से ही हिन्दीं फुटकर रुप में ही सही प्रशासनिक जीवन का हिस्सा थी।फिर हिन्दी की उपयोगिता के सामाजिक सरोकारों के तहत यह स्वतन्त्रता आंदोलन में मुख्य संपर्क भाषा बनी।धीरे-धीरे सांस्कृतिक, आर्थिक, भौतिक, साहित्यिक व प्रशासनिक दुनिया में इसने अपना स्थान बना लिया।
स्वतन्त्रता के पूर्व ही छायावाद में विभिन्न उपन्यासों में,कथासाहित्य में उसके परिमार्जित, अत्यंत व्यंजक, सक्षम और समर्थ भाषा के रूप में दर्शन होने लगते हैं। इसलिए लाख विरोध के बाद भी आजादी के बाद राष्ट्रभाषा के साथ-साथ राजभाषा के दर्जे की भी हिन्दीं ही अधिकारिणी बनी।
आजादी के बाद देश के कार्यव्यहारों में विविधता व संख्यात्मक इजाफा होने के कारण भाषा के कई रुप सामने आए –
- प्रशासनिक हिन्दी
- खेलकूद की हिन्दी
- पत्रकारिता का हिन्दी
- वाणिज्य व्यापार की हिन्दीं इत्यादि।
संपर्क भाषा हिन्दी – आज हिंदी सम्पूर्ण देश में तथा देश के बाहर विदेशों में भी संपर्क भाषा का केंद्र है।हिंदी स्वाधीन भारत में अधिकांश भारतीयों द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा है। इसने बोलचाल के क्षेत्र में अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हिंदी किस तरह संपर्क भाषा के रूप में विकसित होकर जन – मन की अभिव्यक्ति का माध्यम बन रही है इस सन्दर्भ में प्रो. करुणाशंकर उपाध्याय ने लिखा है कि, “अब हिंदी राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा की गंगा से विश्वभाषा का गंगासागर बनने की प्रकिया में है।आज विश्वस्तर पर उसकी स्वीकार्यता और व्याप्ति अनुभव की जा सकती है।आने वाला समय हिन्द और हिंदी का है।इस समय राजनीतिक, समाज –व्यवस्था, धर्म, दर्शन, संस्कृति, पर्यटन, मोरंजन, खेल और रोजगार के क्षेत्र में सबसे प्रभावी भाषा बनकर उभरी है।हमें एकजुट होकर अंग्रेजी के खिलाफ खड़े होना चाहिए। हिंदी और भारतीय भाषाओं को हम शिक्षा का माध्यम बनवाकर अपनी भाषाओं के भविष्य को सदा-सर्वदा के लिए सुरक्षित कर सकतें है।हमें अपनी सरकारों को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि वें शिक्षा का माध्यम हिंदी और भारतीय भाषाओं को रखें और अंग्रेजी दूसरी विदेशी भाषाओं की तरह एक भाषा के रूप में सिखाई जाए।ऐसा करके ही हम आगामी चुनौतिओं के लिए अपने युवाओं को सक्षम, समझदार तथा नवाचार के योग्य बना सकते हैं।तभी वे विश्वस्तरीय मौलिक शोधकार्य कर सकेंगे।यह दौर खुली एवं विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा का है। इस युग का मन्त्र है – ‘स्पर्धा में जो उत्तम ठहरे रह जावें।’ हम अपने नौनिहालों को हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में ही विश्वस्तरीय प्रतियोगिता के योग्य बना सकते हैं।यदि भारत को विश्व गुरु की अपनी स्वाभाविक छवि पुनः प्राप्त करनी है तो यह हिंदी और भारतीय भाषाओं द्वारा ही संभव है।” 1
हमें इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि हिंदी साहित्य में साहित्य सृजन केवल हिंदी भाषा भाषियों ने नहीं किया है बल्कि भारत के लगभग सभी प्रान्तों के साहित्यकारों ने हिंदी में रचनाएं की हैं।सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सुनीतकुमार चटर्जी ने भारतीय भाषाओं के सन्दर्भ में अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहा है कि,” भारत की सभी भाषाओं में हिंदी का स्थान सबसे अधिक है।”
राष्ट्रकवि मैथलीशरण गुप्त ने हिंदी की व्यापकता को कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि, “ हिंदी का उद्देश्य यही है, भारत एक रहे अविभाज्य ,
यों तो रूस और अमरीका जितना है उसका जन राज्य ।
बिना राष्ट्रभाषा स्वराष्ट्र की, गिरा आप गूंगी असमर्थ ,
एक भारती बिना हमारी, भारतीयता का क्या है अर्थ ?”
आज हिंदी की व्यापकता का अनुमान इस संक्षिप्त आंकड़े द्वारा हम लगा सकते हैं कि भारत में हिंदी भाषियों की कुल संख्या 100 करोड़ है इनमें से करीब 50 करोड़ वे लोग हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है।इसके बावजूद वें हिंदी बोल सकते हैं। आज विश्व के 136 देशों के महाविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन – अध्यापन हो रहा है जिससे यह सिद्ध होता है कि वर्तमान समय में विश्व का हर पांचवा या छठा व्यक्ति हिंदी का ज्ञान रखता है।
आज विश्व में 571 मिलीयन लोंगो की मातृभाषा हिन्दी है।
फिजी में 4 लाख लोग
संयुक्त अरब अमिराती – 2 लाख 83 हजार लोग
न्यूझिलंड – 82 हजार
सिंगापूर – 68 मिलीयन
जमैका – 50 मिलीयन
त्रिनिदाद व में 52 मिलीयन
मॅारिशस में -15000 हजार
फ्रैंज गाइना में 6000 लोग हिन्दी को अपनी मातृभाषा मानते है।
इसके अतिरिक्त हिन्दी जानने व समझने वाले लोगों की संख्या 602 मिलियन है।
जो कि विश्व जनसंख्या का 8.3% प्रतिशत है। अंग्रेजी / चीनी के बाद यह तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। स्पेनिश 534 मिलियन के साथ बंगाली चौथे स्थान पर जा चुकी है। बोली जाने वाली अर्थात संपर्क भाषा के रुप में प्रयोक्त की जाती है।इस क्रम में 17 वे नंबर पर आने वाली मराठी भाषा भी क्षेंत्र में यह भाषा लिपि व शब्दकोश को साम्यता के कारण आसान से समझी व बोली जाती है।
बीसवें नंबर पर उर्दू व 23 नंबर को गुजराती की लिपि अलग है,नहीं तो ये तीनों भाषा भाषी सहजता से एक दूसरे की बात को समझ संप्रेषित कर सकते है। 32 नंबर की उड़िया व 33 नंबर की पंजाबी भाषा – भाषियों की भी यही स्थिति है।
वैश्विक भाषाओं में भोजपुरी को अलग भाषा मानकर विश्व में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या के आधार पर उसे 37 वां स्थान दिया गया है। जबकि सचाई यह है कि भोजपुरी हिंन्दी की ही उपभाषा है। बाहरी itenty नहीं। 40वें नं की मैथली व 46 नंबर की अवधी की भी यही स्थिति है।
इसके अतिरिक्त भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर समस्त मिडिल ईष्ट तक हिंन्दी में आसानी संपर्क माध्यम बन जाती है।वह भाषा के रुप में लोगों के बीच बहुराष्ट्रीय संप्रेषण है।
आज अंग्रेजी – 1.452 बिलियन
67 देश की भाषा ही UN, NATO की अधिकृत भाषा है।EU
मंदारिन चीनी – 1.118 बिलियन
हिंन्दी – 343.9 लोगो की मातृभाषा
स्पेनिश – 460 मिलियन लोगो की मातृ भाषा 21 देश की अधिकृत भाषा है।
आर्टिक – 372 मिलियन 25 देश की अधिकृत भाषा है।
फ्रेंच- 300 मिलियन 29 देश की अधिकृत भाषा है।
उर्दू – 170 मिलियन लोगों की मातृभाषा है।
पंजाबी – 125 मिलियन लोगों की मातृभाषा है।
मराठी – 85 मिलियन लोगों की मातृभाषा है।
गुजराती – 61 मिलियन लोगों की मातृभाषा है।
भोजपुरी – 52 मिलियन लोगों की मातृभाषा है।
उड़िया – 35 मिलियन लोगों की मातृभाषा है।
नेपाली – 30 मिलियन लोगों की मातृभाषा है।
इस प्रकार यह मेरे अनुसार विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। और विश्व के बड़े हिस्से में लोग इसे समझ सकते है।वह लगातार वैश्विक विस्तार पा रही है।
प्रशासनिक क्षेत्र में हिंदी–
आज हिंदी राजभाषा का अधिकार पाने के कारण प्रशासनिक क्षेत्र में अपना अधिकार बनाने में प्रयासरत है।वह केंद्र सरकार के सभी विभागों कार्यलयों से लेकर हिंदी भाषी राज्यों के प्रशासनिक कामकाज की प्रमुख भाषा बनती जा रही है।यह भी देखा गया है कि सरकारी कार्यालयों,बैकों, निगमों,निकायों आदि में हिंदी के बोल-चाल के स्वरूप का बहुतायत मात्रा में प्रयोग होता है।हिंदी के माध्यम से सरल सम्प्रेषण सहज ही संभाव्य है क्योंकि यह सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली सम्पर्क भाषा है एवं राष्ट्रीय एकता की सम्पूर्ण कड़ी है।प्राय: देखा गया है कि कार्यालयीन परिप्रेक्ष्य में दैनिक कार्यों में चर्चा के दौरान हिंदी का ही प्रयोग होता है एवं मौखिक निर्देश भी दिए जाते हैं। उच्च स्तरीय बैठकें, बोर्ड मीटिंग, नीति निर्धारण संबधी चर्चाएँ आजकल अधिकांशतया हिंदी में ही देखने को मिलती है। किसी भी सभा, सम्मलेन या संबोधन में अधिकांश उच्चतम अधिकारियों द्वारा भी हिंदी बोली जाती है और योजनाओं को हिंदी में ही समझाया जाता है।हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के सभी संबोधन हिंदी में होते हैं ।यहाँ तक कि केंद्र सरकार की सभी गतिविधियों का माध्यम भौतिक रूप से हिंदी ही होता है।तकनीकी क्षेत्रों में भी परियोजनाओं आदि पर चर्चा करते समय कांट्रेक्टर या कामगारों को हिंदी में समझाया जाता है जिससे वे परियोजना को भलीभांति समझ कर उसे ठीक तरह से निष्पादित कर सकें।
समग्रत: शासन – प्रशासन में, बोलचाल में हिंदी का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हो रहा है। यह सर्वविदित सत्य है कि शासन – प्रशासन के अधिकांश मौखिक आदेश –निर्देश हिंदी में ही दिए जाते हैं।परन्तु लिखित रूप में शासन – प्रशासन में हिंदी की वर्तमान स्थिति में प्रयोग की प्रचुर संभावनाएं हैं।
आज हिंदी राजभाषा का अधिकार पाने के कारण प्रशासनिक क्षेत्र में अपना ठौर बनाने में प्रयासरत है। वह केंद्र सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों से लेकर हिंदी भाषी राज्यों के प्रशासनिक कामकाज की प्रमुख भाषा बनती जा रही है।यह भी देखा गया है कि सरकारी कार्यालयों, बैकों, निगमों निकायों आदि में हिंदी के बोल-चाल के स्वरुप का बहुतायत मात्रा में प्रयोग होता है।
हमारे वर्तमान प्रशासनिक क्षेत्र के सभी संबोधन हिंदी में होते हैं। यहाँ तक की केंन्द्र सरकार को सभी गतिविधीयों के माध्यम भौतिक रुप सें हिंन्दी ही होता है।
जब किसी भाषा को राजकीय संरक्षण प्राप्त होता है तो वह प्रशासन में प्रयुक्त होने लगती है। किन्तु हिन्दी की प्रशासनिक भाषा बनने की कहानी अत्यंत अनूठी है।
भारत में संप्रति 28 राज्य और 8 केंन्द्र शासित प्रदेश है।इनके गठन का मुख्य आधार भाषाई था।हिन्दी चूंकि देश में सर्वव्यापक है और सभी इसको बालते – समझते हैं।इसलिए यह एक लंबे संघर्ष के बाद यह राजभाषा के उच्चपद पर आसीन हो गई किन्तु आजतक भी प्रशासकीय, कार्यालयीन कामकाज पूर्णतः हिन्दी में नही होता है।कार्यालयीन, प्रशासकीय, भाषा की मुख्य विशेषता यह होती है उसका स्वरुप पूर्णतः अभिधात्मक होता है प्रशासकीय, जिससें कोई अन्य अर्थ निकलने की संभावना न हो।हिन्दी का कार्यालयीन स्वरूप विकसित करने में आचार्य रघुवीर सहाय का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने संस्कृत को नवीन पारिभाषिक शब्दावली को आधार के रुप में इस्तेमाल किया। उन्होंने संस्कृत की पाँच सौ धातुऔं,बीस उपसर्गों एवं अस्सी प्रत्ययों से कार्यालयीन अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्दों को स्थानापन्न करने के लिए हिंदी शब्द बनाए।
दूसरी ओर वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने अनुवाद का सहारा लिया।इसके कारण यह भाषा अत्यंत क्लिष्ट हो गई।इसका अंदाज तो डाॅ.रघुवीर को भी होने लगा था इसलिए उन्होंने कहा,’अंग्रेज़ी की प्रत्येक अर्थ-छाया के लिए हिंदी भाषा में भी नया शब्द होना चाहिए। ।।।। अंग्रेजी के तीन शब्द हैं: पहला प्रेरोगेटिव, दूसरा राइट और तीसरा प्रिविलेज।साधारण दृष्टि से ये तीनों एक जैसे शब्द हैं, किंतु प्रयोग की दृष्टि से तीनों अलग- अलग।जब अंग्रेजी में ये तीन शब्द हैं तो हिंदी में भी कम से कम तीन शब्द होने चाहिए (विशेषाधिकार, अधिकार, परमाधिकार)।जो सामान्य लोग हैं उनका तो एक ही शब्द से काम चल जाएगा, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उनको तीन शब्द ही चाहिए।उनका एक शब्द से काम नहीं चलेगा। यह बात चलेगी नहीं।पारिभाषिक शब्दावली तो कभी सरल हो ही नहीं सकती।यह हो सकता है कि बच्चों को सिखाने के लिए आप भाषा सरल कर दें, किंतु पारिभाषिक शब्द सरल नहीं हो सकते।सरल उन शब्दों को कहते हैं जो बिना पढ़े-लिखे लोग, कुली, बच्चे, गाँव के किसान, मजदूर लोग बोलते हैं। जब भी आपके सामने यह बात आये, आप अपने से विचार करें।
*अशोक वाजपेयी अपने व्याख्यानों में अक्सर यह संस्मरण बताते हैं। उन्होंने अपनी रचना ‘हिंदी की बोलियाँ : एक बातचीत’ में सरकारी हिंदी पर संस्कृत के प्रभाव की आलोचना भी की है। देखें, अग्निहोत्री और कुमार, वही: 116-120।
अधिकारियों को समझाइए कि भाषा सरल करने का अर्थ होगा पारिभाषिक भाषा का पारिभाषिकपन समाप्त करना।
डॉ.रघुवीर के विचारों की विस्तार से जानकारी के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय के सहयोग से प्रकाशित उनकी अंग्रेजी में लिखी गयी पुस्तक देखें: रघुवीर, हिंदी की ऊर्जा, अनु। रामचंद्र शर्मा, भगवती प्रकाशन, दिल्ली, 1998; यह उद्धरण उनके एक लेख ‘पारिभाषिक शब्द’ से लिया गया जिसे धर्मवीर ने उद्धृत किया है। देखें, डॉ. धर्मवीर,। बाद में कोशिस की गई कि सरकारी हिन्दी को सरल व सुबोध बनाया जाए पर उसमें अनुदित होने के कारण कृत्रिमता आ गई थी। जो आज भी बरकरार है।
भारत सरकार के राज-भाषा विभाग द्वारा प्रकाशित हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों के संकलन पर निगाह डालने से यह स्पष्ट हो जाता है। सत्तर और अस्सी के दशक में केंद्र सरकार का एक हिस्सा रघुवीरी कारिस्तानी के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए दिखा।गृह मंत्रालय का 1976 में जारी किया गया एक कार्यालय ज्ञापन और फिर 1988 का एक कार्यालय ज्ञापन यह बताता है कि देर से ही सही पर सरकार को अपनी गलती समझ में आ गयी थी।ये ज्ञापन साफ़ तौर से कहते हैं कि सरकारी हिंदी लिखते समय न तो संस्कृत लिखने की कोशिश की जाए और न ही देवनागरी लिपि में अंग्रेजी। अंग्रेजी में मसविदा लिख कर अनुवाद करने के बजाय उसे मूल हिंदी में ही तैयार किया जाए ताकि अनुवाद के अटपटेपन से बचा जा सके। सरकारी हिंदी अलग तरह की नहीं। होती, वह भी सरल और सुबोध होनी चाहिए, उसमें आमफ़हम शब्दों का प्रयोग किया जाए, दूसरी भाषाओं के शब्दों के इस्तेमाल से परहेज़ न किया जाए, समझाने के लिए अंग्रेजी के शब्दों को कोष्ठक में लिख दिया जाए, वाक्य छोटे और सरल बनाये जाएँ। कुछ इसी तरह की हिदायतें केंद्र-राज्य संबंधों पर बने सरकारिया आयोग ने भी दीं। 59 संविधान पारित होने के साठ साल बाद 2011 में भारत सरकार का राज-भाषा विभाग 2011 सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए यह आदेश निकाल पाया है कि सरकारी हिंदी में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी स्रोतों के आमफ़हम शब्दों का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं की जानी चाहिए ताकि सरकारी काम-काज की भाषा सरल और सुबोध बन सके दो उदाहरण
यह कृत्रिमता शब्दावली गठन में नहीं अपिल वाक्य संस्था में भी है। इसलिए इसे अपनाने में प्रैक्टिकल समस्याएं सामने आ जाती है।
सरकारी नौकरी में इतने वर्ष रहने के बाद मेरा अनुभव यह है। कि डीलींग हॅण्ड नवीन ड्राफ्ट बनने में कतराते है। एक वो विषय की जटिलताओं के कारण दुसरा भाषा का अभिधात्मक स्वरुप देने के चक्कर में भाषा का Interpretation कुछ और व हो जाए, इसी कारण ज्यादातर Copy – Paste के माध्यम से मूल ड्राप्ट तैयार करने की प्रवृत्ती रहती है।जिसके कारण समान विषय पर हर प्रकार को संस्थत्मक टिप्पणी पत्र के ड्राफ्ट शब्द समान रहते है। चुंकि अंग्रेजी में पहले से ही देश का सब कामकाज चल रहा था। तो उसी को सुविधाजनक मानते हुए 75 वर्ष बाद तक स्थिती में कोई बदलाव नहीं आ पा रहा है। किंतु यदि हम शब्दावली की और वाक्य विन्याप्त को इस कृत्रिमता और क्लीष्टता को थोड़ा प्राकृतिक व सरल बना पाए तो आज राजनैतिक वातावरण में हिन्दी की स्वीकार्यता कार्यालयीन कामकाज में बढ़ जाएगी।
आजकल केन्द्र सरकार में सभी फाइल्स ई –ऑफिस प्रणाली पर ही होती है। अब वहाँ physical life की संकल्पना शेष नहीं रह गई। अस परिस्थिती में अंग्रेजी में ही टिप्पणी लिखने की बाध्य है। एक तो हिन्दी टाईपिंग आती नहीं। मेरा मानना है कि यदि ई- ऑफिस प्रणाली को हिन्दी में Wookable बनाना है। तो सभी अधिकारिर्यों, कर्मचारियों को हिन्दी में भी की – बोर्ड उपलब्ध करके देना चाहिए और हिन्दी ट्यूटर व टाईप कक्षा पर हिन्दी वर्तनी के विकल्प अंग्रेजी की तरह उपलब्ध होंगे और Word में हिन्दी के लिए भी incorr अशुध्द वर्तनी पर लाल लाइन आएगी तथा उस पर क्लिक करने पर उसके शुध्द विकल्प आएगे तो इससे कार्यालय में दैनंदिन कामों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा।
राजभाषा हिन्दी की एक अन्य समस्या को डॉं भोलानाथ तिवारी में अपनी पुस्तक “राजभाषा हिन्दी” में रेखांकित किया है।“पूरा हिन्दी प्रदेश अपने आप में काफी बड़ा है। बन गया है।
इस संदर्भ में अपने महाराष्ट्र राज्य में काम करने के अनुभव को मैं दर किनार नहीं कर सकती।महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी है। और वह वास्तविक राजभाषा है। चाहे e –office प्रणाली हो या भौतिक संचिकाएं यहाँ फाईलवर्क,बैठकें,अनुदेश ,अधिसूचनाएँ,दिशानिर्देश,नियम,अधिनियम सभी मराठी भाषा में ही हैं। और सभी उनका उपयोग गर्व के साथ करते हैं।
एक तो मराठी भाषियों ने मोड़ी लिपि को त्यागकर नागरी को अपना लिया है।इससे मराठी हिन्दी व संस्कृत की शब्दावलियों का आदान-प्रदान भी आसान हो गया दूसरा फायदा यह हुआ कि मराठी भाषी व्यक्ति के लिए पूरे भारत में काम करनें में कोई खास कठिनाई या बाधा नहीं आती। अगर हम अन्य भारतीय भाषाओं जैसे की गुजराती, मराठी, तमिल, तेलगु, कन्नड, मलयालम, बंगाली, पंजाबी से कुछ शब्दावलियों का आदान – प्रदान करेंगे तो इससे हिन्दी को बढ़ावा मिलेगा। आजकल ग्र मंत्रालय से इस संदर्भ में ने उत्तर – पूर्व के राज्यों की भाषाओं के देवनागरीकरण का बीड़ा उठाया है। यदि यह प्रयास सफल हो गया तो ना केवल भारत की एकता व अखंडता में अधिक मजबूती आएगी बल्कि हिन्दी के व्यापक विस्तार और उसके राजभाषा के रुप में स्थापित करने के सार्थक प्रयासों को और अधिक मजबूती और सफलता प्राप्त होगी।
भोलानाथ तिवारी ने परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला का नमूना अपनी पुस्तक राजभाषा हिन्दी में प्रस्तुत किया है। जिसके प्रयोग लगभग सभी भारतीय भाषाओं के देवनागरी में अभिव्यक्त किया जा सकेगा।
| परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला |
| देवनागरी वर्णमाला |
| स्वरः अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ मात्राएँ: । ि ी ु ू ृ ऋ े ै स्वरः ओ औ अं अः मात्राएँ: े ै ा ा: व्यंजन : क ख ग घ ड च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण ड़ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र हल चिन्ह – \ |
जब हिन्दी व देवनागरी में सभी भाषाओं को अभिव्यक्त करने की नैसर्गिक क्षमता उत्पन्न हो जाएगी तो कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को भी बल प्राप्त होगा।इस काम के लिए कई विभागों ने अपनी परिभाषिक शब्दावलियाँ बना ली है।जैसे विधि न्याय विभाग की विधि शब्दावली और रेल्वे मंत्रालय ने 1978, 79, 81 में अपनी पारिभाषिक शब्दावली की चार पुस्तके प्रकाशित की है।
रिजर्व बॅंक ने 1980 में बॅंकिग शब्दावली प्रकाशित की है। 1973 में आयकर विभाग ने आयकर शब्दावली प्रकाशित की। 1980 में भारतीय साधारण बीमा निगम ने अपनी शब्दावली प्रकाशित की। राजभाषा के रुप में हिन्दी के प्रचार, प्रसार, एकरुपता, लाने के लिए राजभाषा कोश का निर्माण होना चाहिए।
आजकल डिजिटल डिक्शनरी के विकास का काम भी तेजी से चल रहा है। हम मिलकर प्रयत्न करेंगे तो निश्चित ही हिन्दी विश्व की संपन्न व प्रौढ राजभाषा व कार्यालयीन भाषा बन जाएगी।
विधि के क्षेत्र में हिंदी – विधि के क्षेत्र में हिंदी की समस्याएं पारिभाषिक शब्दावली एवं वैधिक सरंचनात्मक भाषा के गठन से जुडी हुई है।इस समय भाषा में भाषा की अभिधात्मकता कार्यलयीन भाषा से भी अधिक होनी चाहिए।
विधि के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को लेकर ब्रिटिशकाल में ही हिंदी की मांग उठने लगी थी।१९वीं शताब्दी में अदालती एवं कार्यालयीन भाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समकक्ष स्थान देने की मांग जोर – शोर से उठाई गई थी।उस समय के नागरिकों और हिंदी भाषी विद्वानों का यह मानना था कि हिंदी को हिंदी को विधि के क्षेत्र की भाषा बना कर ही रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जा सकते है। अतः जब भारतीय संविधान लागू हुआ और उसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तब यह सुनिश्चित हो गया कि हिंदी लगातार विधि के क्षेत्र में भी प्रयुक्त होती रहेगी और विकास के नए आयामों को प्राप्त करेगी।
भारतीय संविधान समितियों में संविधान का प्रारूप तैयार करते समय हिंदी के लिए आफिशियल लैंग्वेज अर्थात् राजभाषा का आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग किया है,तब से अब तक विधि के क्षेत्र में हिंदी का विकास होता जा रहा है वह लगातार विकसित हो रही है।अहिन्दी भाषी क्षेत्र के न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों में भी उसका प्रयोग हो रहा है।हिंदी ने उच्चतम न्यायालय के दरवाजे पर भी दस्तक देकर याचिका स्वीकृत करवा ली है। यह लगातार विधि के क्षेत्र में भी अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा ली है। वैसे तो विधि के क्षेत्र में प्रयुक्त होनेवाली हिंदी लगातार विकसित और फल – फूल रही है। इस समय अनेक संस्थाओं और विद्वानों द्वारा यह मांग भी की जा रही है कि विधि के क्षेत्र में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग हो। इस कारण उच्च न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायलय सब हिंदी को विधि के क्षेत्र में प्रयुक्त होनेवाली एक प्रमुख भाषा के रूप में देखने लगे हैं।अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि के रजिस्ट्रेशन में प्रयुक्त होने वाली उर्दू, फारसी शब्दावलियों के स्थान पर हिंदी शब्दावली के प्रयोग पर जोर देने वाले अधिनियम को पारित किया है।विधि के क्षेत्र में हिंदी की उपयोगिता के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए महात्मा गाँधी ने लिखा है कि, “हमारी कानूनी कार्यवाहियों में हिंदी का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक प्रजा को राजनैतिक कार्यों की जानकारी नहीं मिलेगी।” कहीं न कहीं गाँधी जी द्वारा कही गई बात पर अब अमल किया जा रहा है और वर्तमान में विधि के क्षेत्र में भी हिंदी अपनी उपस्थति दर्ज करा रही है। क्योकि विधि की भाषा भले ही क्लिष्ट हो जाए पर इसमें अर्थ छटाएं नही हो सकतीं।इसमें भाषा के Interpretations भी नहीं हो सकते।हर लिखी बात का एक ही अर्थ निकलना चाहिए।आजादी के समय हिन्दी को राजभाषा का सन्मान मिला,किंन्तु न्यायालयीन भाषा के रुप में देश के उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की भाषा आज भी अंग्रेजी ही बनी हुई है। यदापि जिले स्तर तक न्यायिक व्यवस्थाओं में स्थानीय भाषाओं के प्रयोग को मान्यता दी गई है।
यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348(2) में प्रावधान है, कि राष्ट्रपति से पूर्व सहमति लेकर किसी राज्य के राज्यपाल उस हिन्दी या राज्य की राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही को करने में प्राधिकृत कर सकेगें किन्तु उच्चतम न्यायालय की भाषा हर हाल में अंग्रेजी ही होगी।भारत के विधिआयोग ।इनमे 18 वी रिपोर्ट-(2008)
अभी तक उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेश राज्यों कें राज्यपालों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348/2 के तहत अपने उच्च न्यायालयों में कार्यवाहियों के लिए हिन्दी क प्रयोग को प्राधिकृत कर दिया है। इतना ही नहीं इन राज्यों में उच्च न्यायालय के निर्णयों व आदेशों में हिन्दी का प्रयोग संभव होगा।
अन्य राज्यों ने भी अपने अपने भाषा को उच्च न्यायालय की भाषा के रुप में प्राधिकृत करने का प्रस्ताव भेजा है। एैसे करने वाले राज्यों में है, गुजरात, छत्तीसगढ़, व तमिलनाडु किंतु इनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 के प्रावधान के अनुसार राज्यों के विधान मंडलों में क्रमशः उस राज्य की राजभाषा हिन्दी या अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकेगा।इसके प्रावधान ने हिन्दी भाषी राज्यों में विधी बनाने की भाषा व विधानमंडल की भाषा के रुप में हिन्दी के व्दार खोल दिए है।
विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी–
स्वाधीन भारत में विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को पर्याप्त बढ़ावा मिल रहा है। आज अनेक वैज्ञानिक पत्रिकाएँ हिंदी में निकल रही है।यदि भारत सरकार के विविध वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा वैज्ञानिक पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही है तो दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में ‘विज्ञान प्रकाश’ जैसी उच्चस्तरीय वैज्ञानिक पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में हिंदी विज्ञान एवं प्रद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल में ‘विश्व प्रपंच की भूमिका’ शीर्षक से जर्मन दार्शनिक हेगल की पुस्तक ‘रिडल ऑर यूनिवर्स’ का हिंदी अनुवाद किया जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, प्राणी विज्ञान और शरीर विज्ञान जैसे विषयों पर गंभीर सामग्री उपलब्ध होती है। धीरे- धीरे विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में हिंदी भाषा का प्रयोग बढता गया है आज हिंदी में 4000 से अधिक वैज्ञानिक लेखकों का एक विशाल समुदाय है जिन्होंने 10,000 से अधिक वैज्ञानिक पुस्तकें लिखी है। इस सन्दर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री पी। वी। नरसिंहराव ने लिखा है की, “विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में विदेशी भाषा से कोई राष्ट्र न तो मौलिक ढंग से विकास कर सकता है और न ही अपनी विशिष्ट वैज्ञानिक एवं प्रोद्योगिकीय पहचान बना सकता है।
वर्तमान डिजिटल युग में हिंदी किस तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी उपस्थति दर्ज करा रही है। इस पर विचार करते हुए प्रो.करुणाशंकर उपाध्याय ने लिखा है कि, “आज कोरोना संकट ने प्रोद्योगिकी एवं डिजिटल आधारित शिक्षा पद्धति अपनाने के लिए विवश कर दिया है।हम भलीभांति जानते हैं कि कोरोना कहर से शिक्षा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ है जिसके चलते करोड़ों छात्रों की शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा रहा है।हमें अधिकांश सत्रों की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी और शेष के विकल्प ढूँढने पड़ रहे हैं।बावजूद इसके एक प्राध्यापक होने के नाते हम उत्तरदायित्वों का पूरी निष्ठा से पालन करते हुए तकनीक की सहायता से छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग, सिस्को, वेब एक्स, गूगल मीट, गूगल क्लासरूम, ज़ूम, ई – पाठशाला, यू – ट्यूब रिकॉर्डिंग, टी. सी. एस. आयन क्लासरूम एवं स्मार्ट फोन आदि माध्यमों से हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहें हैं, उनकी कक्षाएं ले रहे हैं।हम आंतरिक मूल्यांकन के कार्य भी ऑनलाइन ही कर रहें हैं। हम ई – कंटेंट अथवा अध्ययन सामग्री भी उन तक पहुंचा रहे हैं इसके अलावा पीएच. डी. के विद्यार्थियों को ऑनलाइन मार्गदर्शन प्रदान कर रहें हैं।आगामी समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे।ऑनलाइन शिक्षण सामग्री कैसे उपलब्ध हो, ऑनलाइन परीक्षाएं कैसे हो,ऑनलाइन पाठ्यक्रम कैसे पढ़ाए जाएं, इस दृष्टि से बड़े परिवर्तन होने की उम्मीद है। वर्तमान विश्व में ज्ञान – विज्ञान के जो नवीनतम साधन और उपल्धियाँ है, उस सन्दर्भ में छात्रों को द्यतन रखना बेहद आवश्यक है इसलिए हम सब तकनीकी साधनों के माध्यम से कार्य कर रहें हैं।आगामी समय तकनीक आधारित शिक्षा व्यवस्था और तकनीक केन्द्रित विश्व- व्यवस्था का साक्षी बनने जा रहा है”।2“वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली नामक जर्नल में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर तथा विज्ञान साहित्य के प्रकाशन में तेरहवें स्थान पर है। शीर्षस्थ विज्ञान संस्थाओं से ८० की सदी शोधकार्य विदेशी पत्रिकाओं में छपते हैं या विदेशी संगोष्ठियों में में प्रस्तुत किए जाते हैं। भारतीय प्रयोगशालाओं में भारत की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध – शोध कार्य को इस तरह विदेशों में प्रकाशित करने से भारत की जनता का कोई लाभ नहीं है, बल्कि इससे अप्रत्यक्षता प्रतिभा पलायन को जोर मिलता है, यह सब टाला जा सकता है, यदि हम सचेत हो जाएं और स्वभाषा का माध्यम अपनाएं। इसके लिए एक पंच सूत्रीय कार्यक्रम निम्लिखित है-
- बदली हुई वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप विज्ञान–प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग हेतु एक उपयुक्त नीति निर्धारित हो एवं कार्यक्रम बने, प्रथमतः यह कार्य संगोष्ठियों के स्तर पर हो।
- तकनीकी हिंदी के प्रयोग–प्रसार व हिंदी में शोध–पत्रादि एवं तकनीकी प्रतिवेदन लेखन पर व्यापक प्रशिक्षण की परियोजना चलाई जाए और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए जाएं।
- देश की अंग्रेजी विज्ञान पत्रिकाओं में अनिवार्यता हिंदी खंड हो तथा सभी अंग्रेजी शोध – पत्रों का सारांश हिंदी खंड में हों तथा सभी अंग्रेजी शोध- पत्रों का सारांश हिंदी में अनिवार्यत: दिया जाए। तकनीकी संगोष्ठियों में हिंदी सत्र की व्यवस्था हो।
- राजभाषा कार्यान्वयन के अंतर्गत वार्षिक कार्यक्रमों में हिंदी में विज्ञान संबंधी प्रशिक्षण, प्रकाशन संगोष्ठी आदि का ब्यौरा शामिल करें एवं तिमाही प्रतिवेदन में ऐसी उपलब्धियों का जिक्र हो।
- विज्ञान–प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी के विविध प्रयोग हेतु उचित प्रोत्साहन की व्यवस्था हो एवं ऐसे कार्यों को उचित मान्यता एवं महत्व दिया जाए”।7
जनसंचार के क्षेत्र में हिंदी–
चूँकि हिंदी भारत वर्ष के सबसे बड़े समुदाय द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा है। अतः जनसंचार के क्षेत्र में भी इसकी विशेष भूमिका रही है। विगत दो शताब्दियों में जनसंचार के क्षेत्र में और वहां प्रयुक्त होनेवाली हिंदी में भी लगातार परिवर्तित हो रही है। जनसंचार के परम्परागत माध्यमों से लेकर आधुनिक माध्यमों तक हिंदी का धडल्ले से प्रयोग हो रहा था। “आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सिनेमा, टीवी, साहित्य – संस्कृति प्रशासन, राज-काज और पाठ्य पुस्तकों द्वारा हिंदी प्रसारित हो रही है। हर माध्यम की अपनी अलग –अलग भाषा शैली है। जन- जन की हिंदी, विज्ञान – तकनीकी, न्याय – पालिका और विदेशियों द्वारा प्रयुक्त हिंदी का भी अध्ययन किया जा सकता है। हमारे अपने देश में तमाम राज्यों और प्रदेशों की अपनी – अपनी बोली भाषा है। इस बोली भाषा के लहजे में प्रयुक्त हों वाली हिंदी भी गजब की है। इन सभी को मिलाकर मुंबई की खिचडीनुमा हिंदी बनती है और अंडरवर्ल्ड की जो टपोरी हिंदी बोली जाती है उसका तो अंदाज ही कुछ निराला है। समाज व्यवस्था में जैसे परिवर्तन होता है वैसे ही समय काल के अनुसार भाषा के स्वरुप में भी परिवर्तन होता रहेगा। कल संस्कृतमय भाषा थी आज यांत्रिकी और तकनीकी से प्रेरित अंग्रेजी मिश्रित हिंदी प्रयुक्त हो रही है। जब बात टेकनोलॉजी की होती है तो अनायास अंग्रेजी का वर्चस्व दिखाई देने लगता है। क्लिष्ट शब्दों के बजाय अंग्रेजी के शब्दों को जस का तस देवनागरी में लिखकर हिंदी के शब्दकोश को बढाया जाना समय की जरुरत है । जैसे- रेल, टेलीविजन, फैक्स, टेलीग्राम , ट्रेन, पोस्ट, बैंक, मोबाइल, कंप्यूटर, रेडियो, टेलिविजन, इंटरनेट,ई-मेल, डाउनलोड, डॉक्टर, ट्रक्टर, मीडिया, यूनिकोड, इंजीनियर, पेपर, प्रिंटर, बटन, इत्यादि, सैकड़ों ऐसे शब्द हैं जो जस के तस रोमन अंगेजी से देवनागरी हिंदी में प्रयुक्त हो रहे है। पहले तो नहीं पर अब धड़ल्ले से इस तरह के शब्दों का प्रयोग रोजमर्रा के जीवन में हो रहा है”3।
सोशल मीडिया की प्रकृति फास्ट फूड की तरह है। इसके कारण हिंदी आलोचना और हिंदी साहित्य जगत पर बुरा प्रभाव भी पड़ा है। इसी तरह कई गलत और अनावश्यक ख़बरें या आर्टिकल्स भी प्रसारित होते है। यह साहित्यिक दुनिया के कन्फेशन जैसा ज्यादा दिखाई देता है। सोशल मीडिया ने नवीन विधाओं वाली नई हिंदी को भी जन्म दिया है जो डिजिटल पव्लिकेशन्स तथा लिट फेस्ट के आयोजन से आच्छादित है। “धीरे – धीरे अब सोशल मीडिया पर साहित्यिक सामग्री आडियो और वीडियो के रूप में भी आने लगी है। यूट्यूब जैसा सोशल मीडिया इसका सशक्त माध्यम है।अक्सर यह भी देखने में आता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई गलत जानकारियां भी प्रसारित होती रहती है जिस पर लगाम लगना जरूरी है। यह किसी के निजी विवेक पर आधारित है। कई बार कुछ ऐसी सामग्री या कविताओं को किसी बड़े लेखक या कवी के नाम पर प्रसारित किया जाता है जिसकी रचना उस लेखक या कवि ने कभी नहीं की जाती है। अपने एक लेख में बालेन्दु शर्मा लिखते हैं कि, ‘सोशल मीडिया साहित्य को नई विधाएं दे सकता है मगर अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। एक ज़माने में ब्लॉगिंग की बड़ी धूम थी। ब्लॉगिंग एक सशक्त विधा बन सकती थी किन्तु वह माध्यम भर बन कर रह गई । अपनी रचना धर्मिता को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम वैसे ही है जैसे कोई भीअन्य माध्यम है या हो सकता है। जैसे टेलिविजन, सिनेमा या नुक्कड़ नाटक साहित्यिक विधाएं अभी भी नहीं है क्योंकि उनके लेखन की कोई स्पष्ट दिशा नहीं है। दूसरी ओर रेडियो नाटक और रिपोतार्ज आदि को देखिए जिनका विधाओं के रूप में पर्याप्त विकास हुआ है। सोशल मीडिया की ही तरह ये भी पारंपरिक माध्यम ही थे किन्तु वे साहित्य के साथ तारतम्य बनाने में सफल रहे।” 4
इस दौर में अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सोशल मीडिया की अपनी अहम् भूमिका है। माना कि यह मान्यता प्राप्त माध्यम नहीं है पर पूरे विश्व में फैला इसका जाल, व्यापकता का एहसास दिलाता है। आज जन-जन के हाथों तक फैला यह एक सशक्त माध्यम है। इसमें एस। एम। एस।, यूट्यूब, वाट्सअप, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, औरकुट, फेसबुक, मैसेंजर, मेल इत्यादि का समावेश किया जा सकता है जो पलक झपकते ही विश्व के एक कोने की खबर दुसरे कोने तक पहुंचा देते हैं। इंटरनेट सोशल मीडिया का प्रमुख माध्यम है। जिसके सहारे यह परिचालित होता है। महज एक क्लिक की सहायता से मिनटों में कोई बात, घटना, साहित्य, संस्कृति, संवाद, तस्वीरें, मनोरंजन, थीम्स, शॉर्ट फिल्म्स, नौकरी के अवसर, विज्ञापन इत्यादि हजारों – हजार लोंगों तक पहुँच जा रहें हैं। इसकी दखल अब चैनल, पत्रकारिता एवं मनोरंजन के अन्य माध्यम भी लेने लगे है। इन माध्यमों में कई भाषाओँ का प्रयोग हो रहा है। अतः हिंदी के पक्ष में बात की जाए तो हिंदी के प्रचार – प्रसार में सोशल मीडिया अहम भूमिका निभा रही है।
“कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ‘मेन्युअल कैसलट’ इसे मास कम्युनिकेशन के बजाय ‘मास सेल्फ कम्युनिकेशन’ का दर्जा देते हैं मतलब हम जनसंचार तो करते है लेकिन जन – स्व – संचार करते है और हमें पता नहीं होता कि हमारा यह संचार विश्व के कितने लोगों तक पहुंचेगा। इस दौर में शार्टकट लिखने के चक्कर में भाषाओं के स्वरूप को बिगाड़ने और एक नई भाषा संस्कृति को जन्म देने में भी सोशल मीडिया मुख्य भूमिका निभा रही है”5 ।
सोशल मीडिया पर हिंदी कई विधाओं में प्रयुक्त हो रही है, जैसे कि यहाँ पर कला, साहित्य, संस्कृति, संवाद, रिपोतार्ज, घटना – प्रसंग इत्यादि का जिक्र किया गया है। हिंदी के स्तर और मानक रूपों की कोई बंदिश नहीं है। भारत में सोशल मीडिया के प्रति बढ़ता क्रेज अब पारंपरिक सामाजिक रिश्तों की नई तस्वीर पेश कर रहा है। इसका प्रयोग छोटे – बड़े, अमीर – गरीब, महिला – पुरुष, सभी वर्ग के लोग कर रहें हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत में फेसबुक इस्तेमाल करने वालों की संख्या अमेरिका से अधिक है। यह जितना लाभदायी है, उतना ही नुकसानदेह भी।
जनसंचार के विविध माध्यमों को हम निम्न रूप में देख सकते हैं-
- लिखित माध्यम – समाचार पत्र – भाषा के विकास, प्रचार – प्रसार में समाचार पत्रों का अप्रतिम योगदान रहता है। हिंदी भाषा के प्रचार – प्रसार और विकास में हिंदी समाचार पत्रों की विशेष भूमिका रही है। हिंदी में प्रकशित पहला साप्ताहिक समाचार पत्र ‘उदन्त मार्तंड’ है जिसे पण्डित जुगलकिशोर मिश्र ने 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित किया था। हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण (1854) भी कलकत्ता में ही प्रकशित हुआ था। उन्नीसवीं सदी में बुद्धि प्रकाश, सत्य दीप, धर्मप्रकाश, तत्वबोधनी, जन प्रकाश, कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, नवभारत, पंजाब केसरी, आज, राजस्थान पत्रिका ने न केवल बीसवीं सदी में प्रकाशवान बनाए रखा बल्कि इक्कीसवीं शताब्दी में भी इनमें से कुछ पत्र अपना परचम लहरा रहें है। प्रसार संख्या की दृष्टि से हिंदी समाचार पत्र अंग्रेजी सहित अन्य सभी भारतीय भाषाओं से काफी आगे है। वर्ष 2016 – 17 में समाचार – पत्रों की कुल संख्या 48,80,89,490 थी जिसमें सबसे अधिक प्रसार संख्या हिंदी समाचार – पत्रों की थी – 28,89,75,773। इस अवधि में अंग्रेजी में प्रसार संख्या 5,24,27,005 थी। किसी एक समाचार पर की प्रसार संख्या की दृष्टि से भी हिंदी आगे है इसमें दैनिक भास्कर की प्रसार संख्या सर्वाधिक है। जबकि दूसरे स्थान पर समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इण्डिया है जिसकी प्रसार संख्या 42,68,703 है।
पत्रिकाएँ – समाचार पत्रों की भांति पत्रिकाएँ भी समाज के विचारों और साहित्य की संवाहिका होती है। पत्रिकाओं में उत्कृष्ट साहित्य मिलता है। हिंदी पत्रकारिता स्वतंत्रता से पूर्व अत्यंत ओजपूर्ण, तेजस्विनी, निर्भय तथा राष्ट्रीय चेतना की संचारिणी रही है। भारतेंदु हरिश्चंद, अम्बिका प्रसाद व्यास, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’ जैसे महान साहित्यकारों ने पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रीय नवजागरण की साधना की। हिंदी पत्रिकाओं से हिंदी की कई साहित्यिक विधाओं की सुरुआत हुई है। राष्ट्रभाषा हिंदी के आन्दोलन में सरस्वती, माधुरी, विशाल भारत, सुधा, हंस, धर्मयुग, और कादम्बिनी आदि पत्रिकाओं का विशेष योगदान रहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी के अलंकारिक और परिष्कृत और व्यवस्थित रूप को साहित्य सृजन में विशेष स्थान दिया जिससे हिंदी भाषा का विकास सत्साहित्य में हुआ।
पत्रिकाओं की संख्या और प्रसार संख्या की दृष्टि से हिंदी में प्रकाशित पत्रिकाओं की संख्या अधिक है। वर्ष 2016 – 17 में 11600 पत्रिकाएँ हिंदी में प्रकशित हुई थी जिनकी कुल प्रसार संख्या 23,89,75,773 थी। जबकि अंग्रेजी में 1487 पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई थी जिनकी प्रचार संख्या 5,65,77,000 थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी में प्रकाशित पत्रिकाओं ने हिदी के प्रचार – प्रसार में अपनी महतवपूर्ण भूमिका निभाई है और अभी भी केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में भी इन पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी भाषा फलफूल रही है।
- श्रव्य माध्यम –
जनसंचार के माध्यमों में भारत में रेडियो का अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्थान रहा है। लेनिन ने कहा था कि “रेडियो बिना कागज़ और बिना दूरी का समाचार पत्र है। डॉ। अर्जुन तिवारी ने लिखा है कि “भारतीय आर्षग्रंथों में नाद ब्रम्हां और शब्द ब्रहम का उल्लेख मिलता है। वेदों में वर्णित है कि ध्वनि से सृष्टि की रचना हुई। ध्वनि में ही ब्रम्हांड का विस्तार होता है तथा ध्वनि में ही वह विलीन हो जाता है।
ध्वनि और शब्द के सामंजस्य का सर्वोत्तम माध्यम रेडियो है। रेडियो मौखिक परंपरा का एक आधुनिक रूप है। भारत में रेडियो का आगमन 23 जुलाई 1927 को ‘हुआ जिसका उद्घाटन इन्डियन ब्राडकास्टिंग कंपनी’ के नाम से तत्कालीन वायसराय ‘लार्ड इरविन’ ने किया है। इसके कुछ बर्ष के उपरांत जब ‘सरदार वल्लभभाई पटेल’ भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री बने तो उन्होंने ने केवल रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अवधि बधाई बल्कि सभी क्षेत्रीय बोलियों कोभी कार्यक्रम रेडियो पर प्रसारित करवाए जिसके कारण ने केवल हिंदी भाषा अपितु क्षेत्रीय बोलियों का भी विकास हुआ और रोजगार के नए मार्ग भी प्रशस्त हुए।
विविध भारती पर प्रसारित कार्यक्रमों की लोकप्रियता निर्विवाद है। भारत सरकार गाँवों का का देश है और यहाँ की अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जहाँ पर आज भी रेडियो संचार का प्रमुख माध्यम है। रेडियो के माध्यम से हिंदी तथा क्षेत्रीय बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित होते है। रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदी का मानक और अखिल भारतीय स्वरुप भी विकसित होता है। इस प्रकार हम कह सकते है कि रेडियो ही लोकतंत्र का संबल और विश्व में विचारों के सम्प्रेषण का एक श्रेष्ठ माध्यम है।
- दृश्य श्रव्य माध्यम –
भारत में टेलिविजन का आगमन 1964 में विक्रम साराभाई के प्रयास से हुआ। आधुनिक संचार क्रान्ति में टेलिविजन की भूमिका अत्यंत महतवपूर्ण है। टेलिविजन किसी राष्ट्र की प्रगति का प्रमाणिक व्याख्याता होता है और राष्ट्र के स्वरुप का दर्पण भी होता है। विगत 10 वर्षों में टेलिविजन ने हमारे जीवन की दिशा बदल दी है। टेलिविजन में प्रसारित कार्यक्रमों के यों तो हर भाषा के दर्शक है परन्तु हिंदी का स्थान उनमें अग्रणी हैं। हिंदी के कार्यक्रम न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी देखें जाते है। आज सामान्यत: 872 से अधिक चैनल है जिनमें से 264 के भी ज्यादा केवल हिंदी के है और कई अहिन्दी चैनलों पर भी हिंदी के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं।
मनोरंजक चैनलों के अलावा समाचार आधारित चैनलों की भी बाढ़ सी आ गई है। देश में 24 से अधिक चैनल 24 घंटों में हिंदी भाषा में ही समाचार प्रस्तुत करते है। इससे हिंदी के विकास और प्रचार प्रसार में टेलिविजन का महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध होता है। टेलिविजन चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों में प्रयुक्त भाषा के स्वरूप पर विचार करने पता चलता है कि जहाँ भाषा की स्वरूपगत विशेषताएं सभी में सामान हैं वहीँ कुछ कार्यक्रम और चैनल विशेष पर भिन्नता भी दृष्टिगोचर होती है। चाहे धारावाहिकों के संवाद की भाषा हो या फिर समाचारों की भाषा हो उनमें हिंदी का नया स्वरूप देखने को मिलता है। टेलिविजन पर प्रसारित इन कार्यक्रमों में हिंदी का जो रूप देखने को मिलता है वह वस्तुतः आधुनिक शिक्षित वर्ग के शहरी परिवेश की हिंदी के रूप को प्रस्तुत करता है। संवादों के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर विकासमान होती आधुनिक हिंदी की झलक मिलती है।
- कम्प्यूटर –
बीसवीं शताब्दी की सबसे क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण उपलब्धि है – कम्प्यूटर। कप्यूटर का सबसे पहले विकास और प्रयोग 1944 में हुआ। द्वितीय विश्वयुद्ध में एटमबम की संबंधित गणनाओं के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया गया और शब्द संसाधनों के लिए अनुसंधान कार्य जोर-शोर से शुरू किए जाने लगे। बीसवीं सदी के नवें दशक में व्यक्तिगत कंप्यूटर के निर्माण से कंप्यूटर के क्षेत्र में एक ऊंची छलांग लगी और इसके साथ विभिन्न भाषाओं के सॉफ्टवेयरों का विकास शुरू हुआ। हिंदी भाषा के भी डास परिवेश में – सुलेख, शब्दरत्न, अक्षर, शब्दमाला जैसे सॉफ्टवेयर विकसित किए गए। किन्तु डास परिवेश में काम करने वालों की अपनी अलग सीमाएं थी। जैसे ही विंडोज का आगमन हुआ कंप्यूटर पर कार्य करने के अनंत द्वार खुल गए। हिंदी के अनेक प्रकार के फॉन्ट आ गए, जो अंग्रेजी के लोकप्रिय सॉफ्टवेयरों में यथा एम।एस वर्ड, एक्सल, पी। पी। टी आदि के साथ अंग्रेजी के साथ सम्मिलित हो गए, अब इनमें हिंदी भाषा में कार्य करना अत्यंत सरल हो गया है।
कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी का प्रयोग बढाने में उनके सॉफ्टवेयरों की विशेष भूमिका रही है जो कंप्यूटर की सहायता से टेलीविजन पर दूसरी भाषाओं के प्रसारित कार्यक्रमों में उपशीर्षक हिंदी में देने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इंटेरनेट के आ जाने से तो सम्पूर्ण विश्व एक छोटे से गाँव में तब्दील हो गया है। दुनिया भर में हिंदी भाषा जानने वालों के लिए इंटरनेट पर हिंदी में बनी बेबसाइटों की उपलब्धता उनके लिए विश्वज्ञान के द्वार बन कर सामने आई है अनेक बेबसाईट हिंदी में उपलब्ध है जिससे हिंदी के प्रचार – प्रसार और विकास को बल मिला है।हिंदी में इमेल भेजने की सुविधा को हम भाषाई कंप्यूटर विकास के क्षेत्र में एक अनुपम उपलब्धि के रूप में देख सकते हैं।
इस प्रकार हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जनसंचार के क्षेत्र में हिंदी स्वंत्रता प्राप्ति के पहले पूर्व अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी थी। जनसंचार के विविध माध्यमों के द्वारा आज भी हिंदी सूचे विश्व में बोली और समझी जा रही है।
तकनीक और हिंदी–
आधुनिक तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी ने अपनी उपस्थिति दृढ़तापूर्वक जब्त कराई है। कम्पूटर के आगमन के साथ ही उस पर हिंदी के प्रयोग को लेकर भी चुनौती उपस्थित हुई । जिसका हिंदी जगत में अच्छी तरह से सामना किया। “हिंदी में सर्वप्रथम कम्पूटर के सन्दर्भ में ही शब्द संसाधन का कार्य प्रारंभ हुआ। यह भाषा संसाधन का आरंभिक सोपान है। किन्तु आरंभिक चरण में रोमन लिपि के माध्यम से ही हिंदी पाठों का कुंजीयन किया जाता था।अब भारत और विदेशों में शब्द संसाधन के अनेक पॅकेज विकसित किए गए है, जिनमें हिंदी में द्विभाषिक रूप से या फिर बहुभाषिक रूप में विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम से शब्द संसाधन के कार्य किए जा सकते हैं। इनमें प्रमुख हैं – अक्षर, मल्टीवर्ड, शब्दमाला, शब्दरतन, बाइस्क्रिप्ट, आलेख, भारती ए। एल। पी। आदि पैकेजों में से कुछ में वे तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध है जो ‘वर्डस्टार’, वर्ड परफेक्ट माइक्रोसॉफ्ट, जैसे अधुनातन वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजों में सुलभ है। किन्तु मात्र शब्द संसाधन से किसी भी भाषा में कंप्यूटर संबंधी महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को संपन्न नहीं किया जा सकता इसलिए भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के सन्दर्भ में कंप्यूटर संबंधी भाषा नीति की घोषणा करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी कंप्यूटर को तभी द्विभाषी मन जाएगा, जब उसमे शब्द संसाधन के साथ – साथ डाटा संसाधन की सुविधा भी हिंदी – अंग्रेजी में, अर्थात द्विभाषिक रूप में उपलब्ध होगी।” 6
डाटा – संबंधी कार्य हिंदी में संपन्न करने के लिए दो विकल्प उपलब्ध है। हार्डवेयर विकल्प और सॉफ्टवेयर विकल्प। जहाँ तक हार्डवेयर विकल्प का सम्बन्ध है, इस दिशा में आई। आई। टी। कानपुर का प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके द्वारा विकसित यह प्रणाली जिस्ट (गेआफिक एंड इंटेलीजेंस बेस्ड स्क्रिप्ट टेकनोलॉजी) प्रोद्योगिकी के रूप में प्रसिद्ध है। इस पर आधारित विभिन्न अनुप्रयोगों के विकास का दायित्व भारत सरकार के सी- डैक नामक संस्थान को सौप गया है।जिसमें परम सुपर कंप्यूटर का विकास भी किया। सी। डैक ( सेंटर पर डेवलपमेंट आफ एडवांस कम्प्यूटिंग) पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। जिस्ट प्रौद्यिगिकी के अंतर्गत पर्सनल कंप्यूटर के मदर बोर्ड पर एक ‘प्लग इन कार्ड’ लगा दिया जाता है। इसी कार्ड को जिस्ट कार्ड कहा जाता है। इस कार्ड की सहायता से आई। बी। एम। पी। सी। कंप्यूटरों पर शब्द संसाधन तथा डाटा – संसाधन के लिए प्रचलित रोमन के सभी पैकेजों का प्रयोग द्विभाषिक या बहुभाषिक रूप में किया जा सकता है। यूनिक्सजेनिक्स परिचालन प्रणालियों के लिए ‘जिस्ट कार्ड’ के बजाय ‘जिस्ट टर्मिनल की आवश्यकता होती है। जिस्ट प्रोद्योगिकी के अनार्गत यह सुविधा सभी भारतीय भाषाओं में सुलभ है और अब यह फारसी, अर्बे, सिंहली, तिब्बती और रूसी लिपि में भी उपलब्ध हो गई है।
इसके विपरीत सॉफ्टवेयर विकल्प के अंतर्गत कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नही होती, ये पॅकेज फ्लापी डिस्क के रूप में उपलब्ध होते हैं। उए पॅकेज दो प्रकार के होते हैं। पहला समर्पित सौफ्टवेयर प्रोग्राम दूसरा सामान्य उद्देश्यीय सौफ्टवेयर परिवेश, समर्पित सौफ्टवेयर प्रोग्राम के अंतर्गत हिंदी में डाटा – संसाधन का एक सॉफ्टवेयर है – ‘देवबेस’( द्विभाषी डाटा बेस प्रबंध प्रणाली) यह सॉफ्टवेयर ही बेस-3 प्लस के अंतर्गत हिंदी में काम करने के लिए यह एक अच्छा पैकेज है। लेकिन जी बेस के संशोधित पॅकेज ( डी – बेस4 ) में हिंदी में काम करने के लिए इसमें संशोधन की आवश्यकता होगी।
सामान्य उद्देश्यीय सॉफ्टवेयर परिवेश के अंतर्गत रोमन लिपि के सभी सॉफ्टवेयर पैकेजों ( जैसे डी। बेस, लोटस, साफ्ट बेस, क्लिपर, फाक्सप्रो, औरेकल आदि।) में हिंदी हिंदी में कार्य किया जा सकता है, उसके अलावा यह परिवेश बेसिक, कोबाल, सी पास्कल आदि प्रोग्रामिंग भाषाओं में तैयार किए प्रोग्रामों में भी हिंदी को आंतरिक क्षमता प्रदान करता है। वस्तुतः यह परिवेश जिस्ट के ही समकक्ष है। जो कार्य जिस्ट के माध्यम से हिंदी में किए जाते है, वें सभी कार्य विकल्प के रूप में इस परिवेश के अंतर्गत भी किए जा सकते हैं। आर। के रिसर्च फाउंडेशन द्वारा विकसित ‘सुलिपि’ नामक यह साफ्टवेयर जिस्ट के सामान ही सामान्य उद्देशीय साफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से एम। एस। डास पर आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर कार्यालय स्वचालन (आफिस आटोमेशन ) अंग्रेजी में साथ – साथ किए जा सकते हैं। जिस्ट व सुलिपि, दोनों के अंतर्गत भारतीय भाषाओं में परस्पर लिप्यांतरण की सुविधा मौजूद है, किन्तु सुलिपि में यह सुविधा हिंदी, पंजाबी, बँगला और गुजराती तक ही सीमित है, जबकि जिस्ट में यह सुविधा सभी भारतीय भाषाओं में सुलभ है।
इसी प्रकार यदि हम हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि हिन्दी एक वैज्ञानिक भाषा है|भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिन्दी को संगणकीय प्रौगरैमिंग की भाषा बनना अत्यन्त सरल है किन्तु इस दिशा में पर्याप्त काम नही हुआ है| भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने हन्दी प्रवाह नाम का सॉप्टवेयर तैयार किया है|
हिदी प्रवाह का भाव पक्ष जितना सबल है, तकनीकी पक्ष भी उतना ही मजबूत है|इस पाठ्यक्रम को भी “लीला पैकेज” प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की भाँति अंग्रेजी के अलावा 14 भारतीय भाषाओं क्रमश: असमिया, बोडो, बांग्ला, गुजराती, कन्नड, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल एवं तेलुगू के माध्यम से जनसाधारण तक ऑनलाइन वेबवर्जन एवं मोबाइल ऐप के रुप में उपलब्ध कराया गया है|
“लीला हिंदी प्रवाह” के वेबवर्जन एवं मोबाइल एवं मोबाइल ऐप में पाठों सें संबंधित शब्दों को समझने एवं समझाने के लिए बृहत शब्दावली का व्यवस्था भी की गई है| इस बृहत शब्दावली में पाठों में सम्मिलित शब्दों के अर्थ यूज़र द्वारा चयनित भाषा, में वर्णक्ररमानुसार दिए गए हैं| इस भाग की विशेषता यह है कि इसमें शब्दों के उच्चारण के साथ-साथ रिकॉर्ड की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है| यूज़र पाठ में आए शब्दों का अर्थ अपनी भाषा में देखने एवं जानने के अलावा हिंदी में उनका उच्चारण सुनने के बाद स्वयं उस शब्द को बोलकर रिकॉर्ड कर सकते है और फिर मूल शब्द एवं स्वंय व्दारा रिकॉर्ड किए हुए शब्द को एक के बाद एक सुनकर उच्चारण संबंधी अपनी कमियों को दूर कर सकते है| यूज़र, अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहे, जितना चाहें और जितनी बार चाहें, इस पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं|
इसी क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने कुछ सुविधाएं प्रदान की हैं-
(a)माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के इंडिक कीबोर्ड (आईएमई) ऐसे ही दो टूल हैं जिनकी मदद से आप बिना किसी खर्च और प्रशिक्षण के कम्प्युटर पर आसानी से टाईपिंग कर सकते हैं और ये आपके सिस्टम पर केवल कुछ सेकंड में इंस्टॉल हो जाते हैं| माइक्रोसॉफ्ट का इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल इसकी तीन सुविधाओं की वजह से बेजोड़ है|
(b) गूगल पर उपलब्ध “ट्रांसलेट” एक अच्छा विकल्प है| यह विविध भाषाओं में अनुवाद हेतु ऑनलाइन सुविधा है और इसके लिए हमें www।translate।google।co।inपर विज़िट करना होता है| वर्तमान में हम गूगल अनुवाद पर उपलब्ध “गूगल टूलकिट” नामक सुविधा पर चर्चा करते हैं| गूगल अनुवादक टूलकिट 8 जून, 2009 में गूगल इंक व्दारा जारी किया गया था|
शब्दकोश
(a) ऑनलाइन शब्दकोश के तहत www।shabdkosh।comएक उपयोगी वेबसाइट है जो हिंदी के अतिरिक्त बांग्ला, गूजराती, कन्नड, मलयालम, तमिल, तेलगू, पंजाबी, मराठी जैसी नौ भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी शब्दों के अर्थ उपलब्ध कराती है|
(b)ई-महाशब्दकोश राजभाषा विभाग व्दारा प्रस्तुत एक ऑनलाइन शब्दकोश है जिसका विकास प्रगत संगणक विकास केंद्र (C-DAC)के व्दारा किया गया है जो कि एक व्दिभाषी- व्दिआयामी उच्चारण शब्दकोश है|
वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का ई–शब्दकोश
(a)वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना सन् 1961 को की गई थी| यह आयोग हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के लिएवैज्ञानिकी एवं तकनीकी शब्दावली का निर्माण एवं समन्वय कार्य के अलावा तकनिकी शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली तथा एन्साइक्लोपीडिया का निर्माण करता है|
(b) हाल ही आयोग अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइल परिभाषिक शब्दावली की सुविधा भी प्रारंभ की है|
हिंदी विश्व की एक विशाल जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है | अत: ऐसे में हमारे यह उत्तरदायित्व अत्यधिक बढ़ जाता है कि हम इसे तकनीक विकास का लाभ देते हुए विश्व की अग्रनी भाषाओं की श्रेणी में स्थापित करने का प्रयास करें|
सूचना प्रौद्योगिकी कम्प्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली का आधार है| सूचना प्रौद्योगिकी, वर्तमान समय में वाणिज्य और व्यापार का अभिन्न अंग बन गयी है| संचार क्रन्ति के फलस्वरुप अब इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक माना जाने लगा है| एक उद्योग के तौर पर यह एक उभरता हुआ क्षेत्र है| इसने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर अक वैश्विक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है| यह नवीन अर्थव्यवस्था अधिकाधिक रुप से सूचना के रचनात्मक व्यवस्था एवं वितरण पर निर्भर है| इसके कारण व्यापार और वाणिज्य में सूचना का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है| इसीलिए इस अर्थव्यवस्था को तूचना अर्थव्यवस्था (Information Economy) या ज्ञान अर्थव्यवस्था (knowledge Economy) भी कहा जाने लगा है|
हिन्दी सिनेमा –
हिन्दी सिनेमा की समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है|भारतीय फिल्म निर्माता-निर्देशकों ने अपनी बेहतर प्रस्तुतीकरण से हिंदी सिनेमा को शिखर पर पहुँचा दिया है| विश्व में सबसे ज्यादा आज हिंदी भाषा में फिल्मों का निर्माण होता है| हिंदी सिनेमा उद्योग ने भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपना एक नजदीकी रिश्ता कायम किया है। देश-दुनिया में हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार में हिंदी सिनेमा का अहम योगदान है| स्पीलबर्ग की फिल्म जुरासिक पार्क ने भारत मे जितना धन अपने हिंदी संस्करण से अर्जित किया वह इसके अंग्रेजी के मूल फिल्म से दो गुना अधिक था| हिंदी भाषा बाजार और मुनाफे की कुंजी बन रही है| आज हॉलीवूड की फिल्म निर्माता भी भारत में अपनी विपणन नीति बदल चुके है| उन्हें पता है की उनकी फिल्में हिंदी में रुपांतरित होने के बाद मूल अंग्रेजी में प्रदर्शित फिल्म से कही अधिक मुनाफा कमा सकती है| पश्चिमी फिल्मों की ब्लॉकस्टर फिल्मों के हिंदी संस्करण की हमारे देश में जितनी खपत होती है वह अंग्रेजी संस्करण की संख्या से अधिक है| भारतीय हिंदी सिनेमा का हिंदी भाषा की व़्यापक लोकप्रियता और इसे संप्रेषण के माध्यम के रुप में आम स्वीकृती दिलाने में अहम योगदान है|हिंदी में बनी फिल्में हिंदी भाषी नागरिकों से ज्यादा अहिन्दी भाषी नागरिकों द्वारा देखी जाती है। हिंदी भाषा के प्रचार – प्रसार में हिंदी सिनेमा के योगदान के विषय में विचार करते हुए दयानंद अवस्थी ने लिखा है कि, “भारतीय हिन्दी सिनेमा को लगभग 106 वर्ष हो गए हैं इस पूरे शतकीय दौर में न जाने कितने विषय आए और कितने विषय गए किन्तु माध्यम का भाषायी ताना बाना हिन्दी भाषा के इर्द गिर्द बुना रहा है। आज हिन्दी भाषा विश्व की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, इथेनोलोग मार्च 2019 के 22वें संस्करण के अनुसार विश्व की दस प्रमुख भाषाओं में (अधिक जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार) चीन की मंदारिन प्रथम, स्पेन की स्पेनिश द्वितीय, ब्रिटेन की अंग्रेजी तृतीय तथा भारत की हिन्दी चतुर्थ स्थान पर है हालांकि क्रमश: पांचवें एवं दसवें स्थान पर भी भारतीय भाषा बंगाली एवं मराठी ही है जिन्होने हिन्दी भाषा के प्रसार पर खूब मदद की है । आज संचार माध्यमों सोशल मीडिया,टेलीविज़न के धारावाहिकों मोबाइल के वेब धारावाहिकों आदि के तीव्र विकास नें इस प्रसार को और अत्यधिक गति दे दी है । ”हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक पुरुषोत्तम अग्रवाल कहते हैं कि भूमंडलीकरण ने भारतीय जीवन को गहरे में जाकर प्रभावित किया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी खत्म हो जाएगी और अंग्रेजी उसका स्थान ग्रहण कर लेगी । वो कहते हैं“भारत की 54 फीसदी आबादी 25 साल से कम उम्र के नौजवानों की है और भूमंडलीकरण ने उसकी आकांक्षाएं और चिंताएं बदली हैं। सूचना और आभासी दुनिया की नागरिकता के धरातल पर किसी कस्बे या महानगर के युवा में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं और रियल टाइम में चैट कर रहे हैं।” इसका जीता जागता उदाहरण है टी वी में दिखाये जाने वाले विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक धारावाहिकों, रियालिटी शो जैसे नृत्य अथवा गायन में समान रूप पूरे भारत के कोने कोने से प्रतिभागियों का अपनी काला कौशल का प्रदर्शन ।
यह संभवत: हिन्दी भाषा के प्रसार का स्वर्णकाल कहा जाएगा जब मनोरंजन के माध्यम से भाषा नें अपनी जड़ें वैश्विक रूप में जमाई है इसमें हिन्दी फिल्मों का योगदान सर्वोपरि माना जाएगा। शायर और गीतकार गुलज़ार ने 8 वें विश्व हिंदी सम्मेलन के तहत ‘हिन्दी के प्रचार प्रसार में हिन्दी फिल्मों की भूमिका’ सत्र की अध्यक्षता करते हुए यह टिप्पणी की थी कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार में फिल्मों ने साहित्य अकादमियों और नेशनल बुक ट्रस्ट से ज्यादा योगदान दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिनेमा, मीडिया और हिन्दी का नाता बहुत पुराना है। जैसे हिन्दी हिन्दुस्तान की जान है, वैसे ही हिन्दुस्तान में हिन्दी के बगैर सिनेमा और मीडिया की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हिन्दी के प्रचार-प्रसार में सिनेमा और मीडिया का योगदान बहुत ही अतुल्य रहा है।हिन्दीतर भाषी क्षेत्रों में सिनेमा और मीडिया ने हिन्दी को जीवनदान दिया है।आज आप भारत के किसी भी कोनें में पहुँच जाएँ वे हिन्दी इसलिए समझ पाते हैं कि उन्होने उसे फिल्मों अथवा अन्य मनोरंजन के माध्यम से देखा व सुना है आज विदेशियों को यदि अपना प्रचार करना होता है, चाहे वह सिनेमा का हो चाहे उनके उद्योग का हो, उन्हें हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी का सहारा लेना ही पड़ता है,भारत में सिनेमा का श्रीगणेश दादा साहब फाल्के द्वारा 1912 में निर्मित और 1913 में प्रदर्शित रजा हरिश्चंद फ़िल्म से माना जाता है। इसके उपरांत प्रथम वाक फ़िल्म आलामारा का निर्माण 1931 में हुआ था तब से लेकर आज तक भारत में असंख्य फिल्मों का निर्माण हो चुका है। जन सामान्य में हिंदी को लोकप्रिय बनाने का महत्वपूर्ण योगदान हिंदी सिनेमा को दिया जा सकता है। भारत में अपनी शैशवावस्था से ही हिंदी के विकास और प्रसार में फिल्मों ने अहम् भूमिका अदा की हैं। सन 1931 में 27 फिल्में बनी थी जिनमें से 22 फिल्में हिंदी में बनी थी। भारत में प्रतिवर्ष 1000 फिल्में बनती हैं जिनमें से सबसे अधिक संख्या हिंदी फिल्मों की होती है। हिंदी फिल्मों भाषा में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक प्रचलित विभिन्न भाषाओं – बोलियों के शब्द सहज रूप से मिलते हैं अधिकांश हिंदी फिल्मों का निर्माण अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में होता है जो हिंदी के व्यापक प्रचार और उसकी लोकप्रियता को सिद्ध करता है। यदि हम हिंदी सिनेमा के साथ – साथ टेलिविजन की बात करें तो हिंदी के प्रचार – प्रसार में टी। वी पर प्रसारित किए जाने वाले धारावाहिक अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहें है। शहरों से लेकर छोटे गांवों तक के लोग जो कि वहां बोली जाने वाली क्षेत्रीय बोली से ही परिचित थे अब उन्हें हिंदी का ज्ञान भी हो गया है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि हिंदी सिनेमा का हिंदी भाषा के प्रचार – प्रसार में अत्याधिक योगदान है।
निष्कर्ष
सारांश यह है कि स्वाधीन भारत में लगातार हिंदी भाषा का विकास हो रहा है। वह सभी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है।हिंदी अब भारतीय उपमहाद्वीप में संपर्क भाषा बन गई है।वह राजभाषा होने के कारण शासन, विधि, विज्ञान और तकनीक सभी क्षेत्रों में प्रयुक्त हो रही है । वह जनसंचार माध्यमों की प्रमुख भाषा बन कर उभरी है।आज हिंदी सिनेमा हजारों करोड़ का व्यापार कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं की हिंदी सिनेमा और मीडिया के क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय और उपयोगी भाषा बन गई है। संक्षेप में हिंदी उन तमाम क्षेत्रों में प्रयुक्त होने के कारण लगातार विकसित और समृद्ध हो रही है। आज उसका वैश्विक विस्तार बेहद आश्वस्तिकारक है।
संदर्भ सूची
- भाषा पत्रिका (द्वैमासिक ), मार्च – अप्रैल 2021, वर्ष -60, अंक -2, पृष्ठ संख्या – 14 -15
- वही पृष्ठ संख्या – 10
- प्रौद्योगिकी बैंकिंग और हिंदी, पृष्ठ संख्या- 101 , रमेश यादव
- वही.
- वही.
- भाषा : राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी, डॉ. डी. सत्यलता, पृष्ठ संख्या 236
- वही.
- साहित्य सिनेमा सेतु पत्रिका ( रील से रियल तक ) ISSN : 2584-0819, लेख – ‘ हिंदी सिनेमा में हिंदी का बदलता स्वरुप’